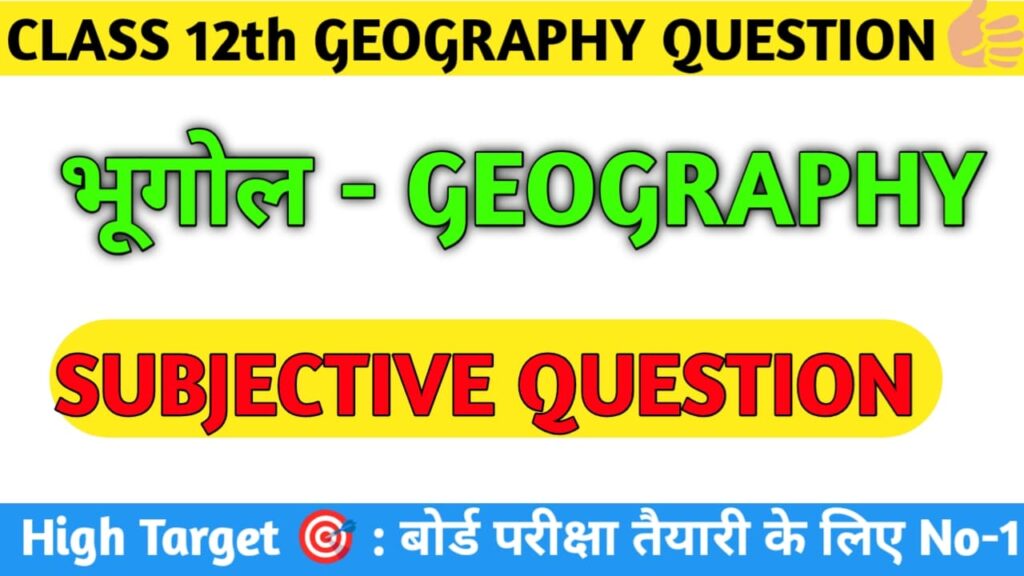प्रश्न 1. पर्यावरण प्रदुषण किसे कहते है ?
या
प्रदुषण किसे कहते है ?
उत्तर – वातावरण में मौजूद हवा, पानी, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जेविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन, जिससे जिव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो उसे पर्यावरण प्रदुषण कहते है |
इस प्रकार प्रदुषण के जिम्मेदार पदार्थ को प्रदुषण कहते है |
प्रश्न 2. प्रदूषक किसे कहते है ?
उत्तर – वातावरण की स्थिति में नाकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ के रूप को प्रदूषक कहते है |
अर्थात पर्यावरण में प्रदुषण उत्पन्न करने वाले जिम्मेदार पदार्थ को ही पदार्थ प्रदूषक कहते है |
प्रश्न 3. प्रदूषक एवं प्रदुषण के बिच अंतर स्पष्ट करे ?
उत्तर –
प्रदूषक (Pollutant):
प्रदूषक वह कोई भी पदार्थ या चीज़ होती है जो हमारे पर्यावरण (जैसे हवा, पानी, जमीन) को गंदा या नुकसान पहुँचाती है। उदाहरण के लिए — धुआँ, जहरीली गैसें, प्लास्टिक कूड़ा, रासायनिक पदार्थ आदि।
प्रदूषण (Pollution):
प्रदूषण वह स्थिति है जब हमारे पर्यावरण में प्रदूषक की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वह वहां के जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। यानी प्रदूषण, प्रदूषक के कारण होने वाला परिणाम है।
आसान शब्दों में:
प्रदूषक वो चीज़ है जो पर्यावरण को गंदा करती है।
प्रदूषण वह समस्या है जो प्रदूषक के कारण पैदा होती है।
प्रश्न 4. वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए ।
उत्तर – वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत
वायु प्रदूषण होने के पीछे कई कारण होते हैं। इनमें सबसे बड़े कारण हैं:
कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना
कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें
खनन (खनिज निकालने) का काम
इन सभी कारणों से हवा में कई हानिकारक गैसें और ज़हरीले पदार्थ जैसे सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और एस्बेस्टस फैल जाते हैं। ये सब हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं।
प्रश्न 5. भारत में नगरीय अपशिष्ट से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए ।
उत्तर – भारत के शहरों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ कचरे की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। लोग जहाँ-तहाँ कूड़ा-कचरा फेंक देते हैं, जिससे शहर गंदा दिखने लगता है। ठोस अपशिष्ट यानी प्लास्टिक, पॉलीथिन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के टूटे-फूटे हिस्से, कांच, कागज, और मकानों के मलबे ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। इन कचरों का सही ढंग से निपटारा करना बहुत जरूरी है, वरना इससे शहर का वातावरण और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा।
प्रश्न 6 .मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं?
उत्तर – जब कोयला, पेट्रोल, और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं, तो औद्योगिक कारखानों से और खनन के कामों से हवा में बहुत सारी जहरीली गैसें और धूल फैलती है। इनमें सीसा और अन्य खतरनाक कण भी होते हैं, जो हवा को गंदा और प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रदूषित हवा से इंसान के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़े, दिमाग और खून से जुड़े कई रोग हो सकते हैं।
प्रश्न 7. भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए।
उत्तर – जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव
भारत में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते उद्योगों की वजह से पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इससे नदियाँ, नहरें, झीलें और तालाब गंदे हो गए हैं। पानी में कई तरह की मिलावट होती है जैसे मिट्टी के कण, और रासायनिक पदार्थ। जब ये पदार्थ पानी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो पानी प्रदूषित हो जाता है और खुद से साफ़ नहीं हो पाता। ऐसा पानी इंसान और जीव-जंतुओं के लिए नुकसानदायक हो जाता है।
जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत:
औद्योगिक कचरा: कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, जहरीली गैसें, और भारी रासायनिक तत्व पानी में मिल जाते हैं।
खेती में रासायनिक पदार्थ: उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक जो बारिश या सिंचाई के पानी के साथ नदियों और जमीन में पहुंच जाते हैं।
धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ: तीर्थयात्रा, पूजा-पाठ और पर्यटन से भी पानी गंदा होता है।
इन कारणों से भारत के लगभग सभी पानी के स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं और पीने या इस्तेमाल के लायक नहीं रहे।
प्रश्न 8. भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर – भारत के शहरों में एक तरफ़ तो बड़ी-बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और अच्छी सुविधाएँ होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ झुग्गी-बस्तियाँ, गंदी कॉलोनियाँ और रेलवे पटरियों के किनारे झोपड़ियाँ भी होती हैं। इन झुग्गियों में ज़्यादातर वे लोग रहते हैं जो गाँवों से रोज़गार की तलाश में शहरों में आए होते हैं। ये लोग महँगे मकान या ज़मीन खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए मजबूरी में ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ बुनियादी सुविधाएँ नहीं होतीं।
इन बस्तियों में:
घर टूटे-फूटे और कमजोर होते हैं
पीने का साफ पानी, रोशनी, शौचालय और साफ-सफाई की सुविधा नहीं होती
सड़कें बहुत संकरी और भीड़-भाड़ वाली होती हैं
आग लगने या बीमारियाँ फैलने का ख़तरा ज्यादा होता है
यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर शहरों में असंगठित काम (जैसे दिहाड़ी मज़दूरी) करते हैं। इन्हें कम पैसे मिलते हैं और काम भी जोखिम भरा होता है। इस वजह से ये लोग कुपोषण, बीमारी, अशिक्षा और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर गरीबी के कारण कुछ लोग नशा, अपराध और समाज से दूर होने जैसी समस्याओं में भी फँस जाते हैं।
प्रश्न 9. भू-निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए ।
उत्तर – भू-निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की उपजाऊ ताकत यानी उत्पादकता में धीरे-धीरे या अचानक कमी आना। यह कमी स्थायी या अस्थायी भी हो सकती है।
भू-निम्नीकरण के कारण
🔹 1. प्राकृतिक कारण:
रेगिस्तान और रेतीली तटीय ज़मीन
पथरीली और पहाड़ी इलाके
ढलान वाली ज़मीन
हिम से ढके क्षेत्र
👉 ये ज़मीनें प्राकृतिक रूप से खेती के लायक नहीं होतीं।
🔹 2. मानवजनित कारण (इंसानों द्वारा पैदा किए गए):
ज़मीन का बार-बार और बिना आराम दिए इस्तेमाल
ज़मीन की खराब देखभाल (कुप्रबंधन)
मिट्टी का कटाव (मृदा अपरदन)
ज़मीन में बहुत ज्यादा पानी भर जाना (जलाक्रांतता)
मिट्टी में नमक या क्षार की मात्रा का बढ़ना (लवणता व क्षारीयता)
भारत में स्थिति:
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 17.98% हिस्सा बंजर और निम्नीकृत भूमि है।
इनमें:
पहाड़
पठार
खड्ड
रेतीले और मरुस्थली इलाके शामिल हैं।
समाधान (भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के उपाय):
नई तकनीकों और खेती की आधुनिक विधियों से कुछ ज़मीन को फिर से खेती लायक बनाया जा सकता है।
रेतीली और तटीय ज़मीन में उर्वरक, जैविक खाद (कम्पोस्ट) और सिंचाई सुविधा देकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है।
दलदली या पानी से भरी ज़मीन को अच्छे प्रबंधन से उपजाऊ बनाया जा सकता है।

SANTU KUMAR
I am a passionate Teacher of Class 8th to 12th and cover all the Subjects of JAC and Bihar Board. I love creating content that helps all the Students. Follow me for more insights and knowledge.
Contact me On WhatsApp