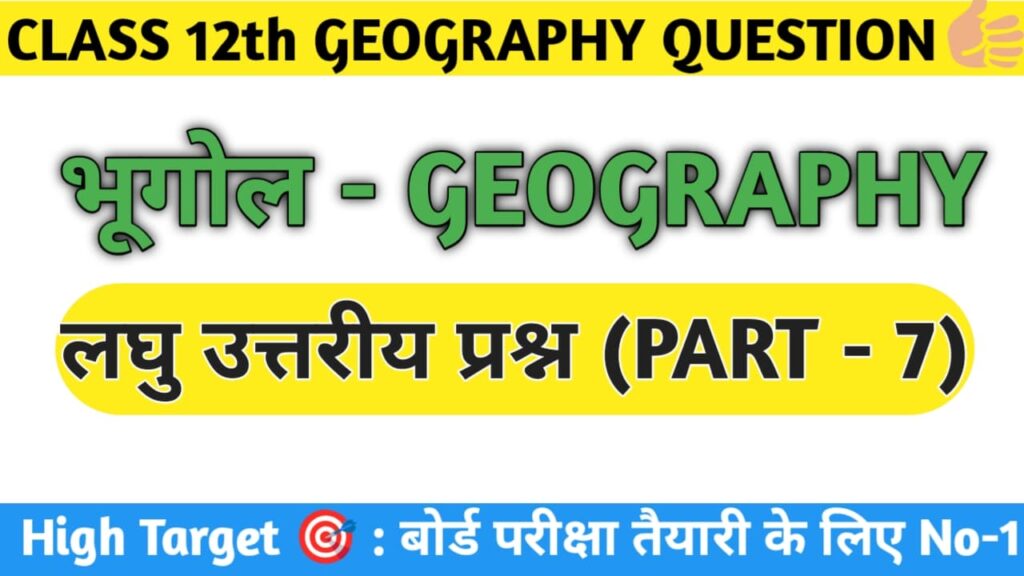121. भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले पाँच राज्यों के नाम बताइये।
उत्तर – भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले पाँच राज्यों के नाम और उनकी जनसंख्या इस प्रकार हैं:
उत्तर प्रदेश – 19.96 करोड़
महाराष्ट्र – 11.24 करोड़
बिहार – 10.38 करोड़
पश्चिम बंगाल – 9.13 करोड़
आंध्र प्रदेश – 8.43 करोड़
यह जनसंख्या आँकड़े भारतीय राज्यों की जनसंख्या वितरण को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
122. सतलज-गंगा के मैदान में सघन जनसंख्या के संकेंद्रण के कारणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर – सतलज-गंगा के मैदान में स्थित राज्य और उनके जनसंख्या घनत्व के बारे में जानकारी इस प्रकार है:
राज्य: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल
विशेषताएँ:
ये सभी समतल मैदान हैं, जहां उर्वर मिट्टी और सदावाहिनी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना और सतलज जल संसाधन प्रदान करती हैं।
उपयुक्त जलवायु और कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इन राज्यों में कृषि विकास को बढ़ावा देती हैं।
सड़क, रेल और जलमार्ग का अच्छा नेटवर्क भी इस क्षेत्र में जनसंख्या के संकेंद्रण में सहायक है।
दिल्ली और कोलकाता के नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी छोर पर स्थित हैं, जो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी):
दिल्ली: 9340 (सबसे अधिक)
पश्चिम बंगाल: 903
बिहार: 880
उत्तर प्रदेश: 690
पंजाब: 484
हरियाणा: 477
इस क्षेत्र में जनसंख्या का विशाल संकेंद्रण इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ कृषि और औद्योगिकीकरण दोनों का अच्छा संतुलन है, और संचार व्यवस्था भी अत्यधिक विकसित है।
123. प्रत्येक उत्तरोत्तर जनगणना में जनसंख्या का घनत्व क्यों बढ़ रहा है ?
उत्तर – जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो स्थिर रहता है, अर्थात् इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में होने वाली जनगणना के साथ निरंतर बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि हो रही है।
उदाहरणस्वरूप, वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 84.63 करोड़ थी, और उस समय जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद 2001 में जनसंख्या बढ़कर 102.86 करोड़ हो गई, जिससे घनत्व भी बढ़कर 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इस प्रकार, जनसंख्या में वृद्धि का सीधा प्रभाव जनसंख्या घनत्व पर पड़ता है।
124. गैरिसन या छावनी नगर क्या होते हैं? उनका क्या प्रकार्य होता है ?
उत्तर – गैरिसन नगर, जिन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है, वे विशेष नगर होते हैं जहाँ सेना की टुकड़ियाँ तैनात रहती हैं और उनके शस्त्रों व अन्य सैन्य साजो-सामान का भंडारण किया जाता है। इन नगरों की स्थापना मुख्यतः देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की जाती है।
भारत में अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर आदि प्रमुख छावनी नगर हैं। इनका प्रमुख कार्य सैनिकों को एक सुरक्षित, अनुशासित और उपयुक्त वातावरण प्रदान करना होता है, जिससे वे हर स्थिति में सतर्क और तैयार रह सकें। साथ ही, यहाँ सैन्य सामग्री के भंडारण, प्रशिक्षण और संचालन की उपयुक्त व्यवस्थाएँ होती हैं।
इन नगरों का देश की सामरिक सुरक्षा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।
125. महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं ?
उत्तर – महानगर उन नगरों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के मध्य होती है। ये नगर अपने आकार, जनसंख्या और सुविधाओं के कारण शहरीकरण के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। महानगरों को नगरीय संकुल (Urban Agglomeration) से अलग माना जाता है। नगरीय संकुल में प्रायः एक बड़ा मुख्य नगर (महानगर या मेगानगर) शामिल होता है, जिसके साथ उसका बहिर्वृद्ध (Outgrowth), संपर्क नगर (Satellite Town) अथवा संपर्क प्रसार नगर भी सम्मिलित होते हैं। दूसरी ओर, महानगर स्वयं एक स्वतंत्र नगरीय इकाई हो सकता है, और इसके साथ किसी संपर्क नगर या बहिर्वृद्ध का होना अनिवार्य नहीं होता। इस प्रकार, नगरीय संकुल एक समग्र शहरी क्षेत्र होता है, जबकि महानगर एक विशिष्ट, बड़े आकार का अकेला नगर भी हो सकता है।
126. भारत में कौन-से क्षेत्र मानव आवास के लिए आकर्षक नहीं है?
उत्तर – भारत में पर्वतीय, मरुस्थलीय और वनाच्छादित क्षेत्र सामान्यतः मानव निवास के लिए अनाकर्षक माने जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आदि में धरातल ऊबड़-खाबड़ और असमतल होता है, जिससे वहाँ घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढाँचों का निर्माण कठिन हो जाता है। साथ ही, इन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं की भी कमी होती है। मरुस्थलीय भागों में जल की भारी कमी, सीमित वनस्पति, शुष्क जलवायु और अत्यधिक तापमान के कारण मानव निवास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार, वनाच्छादित क्षेत्रों में घने जंगल, दलदली भूमि और अन्य भौतिक बाधाएँ निवास को कठिन बना देती हैं। इन क्षेत्रों तक पहुँचना भी चुनौतीपूर्ण होता है। इन्हीं कारणों से ये क्षेत्र मानव निवास के लिए अपेक्षाकृत कम आकर्षक माने जाते हैं।
127. शुष्क कृषि किसे कहते हैं?
उत्तर – शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो कम जल में भी पनप सकें और शुष्कता को सहन कर सकें। ऐसी फसलों में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार आदि प्रमुख हैं। शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में मृदा में नमी बनाए रखना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे– मेड़बंदी, मल्चिंग, कंटूर प्लाउइंग आदि। यह पद्धति उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ सिंचाई की सीमित व्यवस्था है और खेती मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है।
128. पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं ?
उत्तर – पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य भौम जल (Groundwater) के अत्यधिक उपयोग के लिए जाने जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये राज्य कृषि के दृष्टिकोण से अत्यंत विकसित हैं, और कृषि का विकास मुख्य रूप से सुव्यवस्थित सिंचाई तंत्र पर निर्भर करता है।
इन राज्यों में निवल बोया गया क्षेत्र लगभग 85% तक सिंचित है। यद्यपि नहरों के माध्यम से सिंचाई भी इन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भी कुएँ और नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, जो भौम जल पर आधारित होते हैं।
पंजाब में निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1%
हरियाणा में 51.3%
और तमिलनाडु में 54.7% भाग कुओं और नलकूपों से सिंचित होता है।
इस प्रकार, इन राज्यों में भौम जल का दोहन सर्वाधिक होता है, जिससे इनका भौम जल विकास स्तर बहुत ऊँचा है।
129. देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना – क्यों है?
उत्तर – वर्तमान समय में भारत में जल उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र के खाते में जाता है। कृषि क्षेत्र में धरातलीय जल का लगभग 89% और भौम जल का 92% उपयोग किया जाता है, जो इसे जल उपभोग का सर्वाधिक उपयोगकर्ता बनाता है।
इसके विपरीत,
औद्योगिक क्षेत्र में केवल 2% धरातलीय जल और 5% भौम जल का उपयोग होता है,
जबकि घरेलू क्षेत्र में 9% धरातलीय जल और 3% भौम जल का ही उपयोग होता है।
हालाँकि वर्तमान में कृषि जल उपयोग में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, फिर भी भविष्य में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, और औद्योगिकीकरण के चलते औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्रों में जल की माँग में वृद्धि होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, कुल जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का अनुपात घट सकता है, और जल संसाधनों पर बहु-क्षेत्रीय दबाव बढ़ेगा।
130. भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी दो कारकों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर – भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के सभी क्षेत्रों में जल की माँग निरंतर बढ़ रही है। विशेष रूप से सिंचाई क्षेत्र में जल की माँग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में धरातलीय जल का लगभग 89% और भौम जल का 92% भाग कृषि एवं सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।
इसी अत्यधिक उपयोग के कारण भारत में जल-संसाधनों की उपलब्धता में तेज़ी से कमी आ रही है।
उदाहरण के लिए:
वर्ष 1951 में देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 5177 घन मीटर थी।
यह घटकर 2001 में 1829 घन मीटर रह गई।
यदि यही स्थिति बनी रही, तो अनुमान है कि 2025 तक यह और घटकर 1342 घन मीटर पर पहुँच जाएगी।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो जाती है, तो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इस स्थिति से बचने के लिए जल संरक्षण, कुशल जल प्रबंधन तथा वैकल्पिक सिंचाई तकनीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
131. जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है। क्यों?
उत्तर – भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती माँग और जल के असमान वितरण के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार गिरावट हो रही है। केवल मात्रा ही नहीं, जल की गुणवत्ता भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सीमित जल संसाधन अब औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू निस्सरणों (effluents) से प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे उपयोगी जल की उपलब्धता और भी सीमित होती जा रही है। वर्तमान में भारत में लगभग 90% जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश के अधिकांश राज्यों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कृषि उत्पादन को बनाए रखा जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में, जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि उपभोक्ताओं को भविष्य में संतुलित एवं पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, तो हमें जल के सतत उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।
132. बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर – बंजर या ऊसर भूमि उन सभी प्रकार की भूमियों को कहा जाता है जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ, अनुपयोगी और बेकार होती हैं, तथा वर्तमान प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकतीं। इनमें बंजर पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, बीहड़ (ravines) आदि भू-भाग शामिल हैं।
इसके विपरीत, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि होती है जो स्वभावतः उपजाऊ होती है और कृषि योग्य भी है, परंतु कुछ भौगोलिक व पर्यावरणीय कारणों से जैसे—
जंगली पौधों व घासों का अत्यधिक विकास,
जल-जमाव,
मिट्टी अपरदन (erosion),
आबादी से अधिक दूरी आदि,
यह भूमि पिछले पाँच वर्षों या उससे अधिक समय से परती (unused) पड़ी रहती है।
इस प्रकार की भूमि को भूमि उद्धार तकनीकों जैसे– जल निकास सुधार, मिट्टी संरक्षण, वृक्षारोपण आदि द्वारा सुधार कर फिर से कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
133. पश्चिम बंगाल में जूट की कृषि का वर्णन कीजिए।
उत्तर – भारत की छाल वाली रेशेदार फसलों में जूट सबसे प्रमुख है, जिससे रस्सी, टाट, बोरा, गलीचा आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। जूट के पौधे लगभग 2 से 4 मीटर ऊँचे होते हैं। जब पौधों को काटा जाता है, तो उन्हें पानी में सड़ने के लिए डाला जाता है। इस प्रक्रिया के बाद उनकी छाल को अलग किया जाता है, और फिर उसे पीटा जाता है, जिससे उसमें से रेशे निकल आते हैं। इन रेशों की बिक्री होती है, और इसलिए जूट को एक नकदी फसल माना जाता है। जूट उद्योग में यह कच्चा माल इस्तेमाल होता है। जूट उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है और इसकी खेती के लिए 25 से 30° C तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और डेल्टाई मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट को सड़ाने के लिए तालाब या जलाशय की आवश्यकता होती है। भारत में जूट उत्पादन का मुख्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, जो इस फसल के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त है। इस राज्य को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश का दो-तिहाई जूट उत्पन्न होता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर जूट की खेती की जाती है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र राज्य के पूर्वी भाग में, हुगली नदी के किनारे स्थित हैं। मुर्शिदाबाद, दीनाजपुर, कूच बिहार, हुगली, 24 परगना, नादिया, जलपाईगुड़ी, माल्दा, बर्द्धमान, और हावड़ा जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।
134. विशेषीकृत फलोत्पादन एवं सब्जी वाली कृषि शहरों के निकट विकसित होती है। क्यों ?
उत्तर – शहरों में जनसंख्या की अधिकता के कारण फलों और सब्जियों की माँग बहुत बढ़ जाती है। चूँकि फल और सब्जियाँ शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पाद होते हैं, इन्हें दूर से लाने पर इनके खराब होने का जोखिम रहता है। इस कारण, शहरों के निकट इनकी खेती की जाती है ताकि ताजे उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकें। हालाँकि, यातायात के तीव्र साधनों के विकास ने इन उत्पादों को दूर-दूर से लाने में सुविधा प्रदान की है, और अब इनकी खेती शहरों से दूर भी की जा सकती है। फिर भी, ताजा फल और सब्जियाँ आमतौर पर निकटवर्ती क्षेत्रों पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि ताजे उत्पाद की माँग लगातार बनी रहती है और शहरों में इन्हें जल्दी पहुँचाना आवश्यक होता है।
135. शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अन्तर है ?
उत्तर – शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इस पद्धति में, वर्षा की कमी के कारण ऐसी फसलों की खेती की जाती है, जो शुष्कता को सहन कर सकती हैं, जैसे- रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण और वर्षा जल संचयन की विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं ताकि जल का उचित उपयोग किया जा सके और फसलों का उत्पादन बढ़ सके। इसके विपरीत, आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा ऋतु में जल की अधिकता होती है और पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में उन फसलों की खेती की जाती है जिन्हें अधिक पानी चाहिए, जैसे- चावल, जूट, गन्ना इत्यादि।
136. भारतीय कृषि की तीन विशेषताओं को लिखिए।
उत्तर – भारतीय कृषि की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं:
गहन निर्वाहक कृषि (Intensive Subsistence Farming): भारत में अधिकांश किसान अपनी खुद की आवश्यकता के लिए कृषि करते हैं, और कृषि की यह पद्धति अधिक श्रम-प्रधान और कृषि भूमि के छोटे आकार पर आधारित होती है।
वर्ष में तीन मौसमी फसलें: भारत में तीन मुख्य फसलें उपजायी जाती हैं, जो हैं:
खरीफ फसल (मानसून के दौरान): जैसे धान, मक्का, सोया।
रबी फसल (सर्दी के मौसम में): जैसे गेहूं, जौ, चना।
जायद फसल (गर्मियों में): जैसे मूँग, उबाली धान, तरबूज आदि।
वर्षा पर निर्भरता: भारतीय कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित होती है, और मॉनसून के समय की बारिश से कृषि उत्पादन निर्धारित होता है। अत्यधिक वर्षा या कमी दोनों ही कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं।
137. गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए ?
उत्तर – गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, और इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं:
दीर्घकालीन ग्रीष्मऋतु: गन्ने की खेती के लिए ग्रीष्मऋतु (गर्म मौसम) का होना आवश्यक है, जिसमें तापमान 21° C से 27° C तक हो।
कम से कम 150 सेमी वार्षिक वर्षा: गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा का होना जरूरी है, या फिर सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए।
पर्याप्त धूप और पाले से रक्षा: गन्ने को अच्छी धूप की आवश्यकता होती है, और पाले (ठंड) से सुरक्षा भी जरूरी होती है, क्योंकि पाले से फसल को नुकसान हो सकता है।
उपजाऊ दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी: गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और हल्की चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिससे फसल की अच्छी वृद्धि हो सके।
पर्याप्त सस्ते मजदूर: गन्ने की खेती मजदूरी की मांग करती है, इसलिए सस्ते और पर्याप्त मजदूर उपलब्ध होने चाहिए।
138. ऋषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है । स्पष्ट करें ।
उत्तर – भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। यही कारण है कि भारत की कामगार जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है। वर्तमान में, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2 प्रतिशत हिस्सा कृषक और कृषि मजदूर हैं। इसके विपरीत, केवल 4.2 प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में कार्यरत हैं, जबकि 37.6 प्रतिशत श्रमिक अन्य गैर-घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, और अन्य सेवाओं में कार्य करते हैं।
139. उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं?
उत्तर – उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन नहर, कुआँ और नलकूप हैं। इनमें नहर द्वारा सिंचाई का विशेष महत्व है।
उत्तर भारत के कुछ प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और बिहार में नहरों, कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके पीछे के कारण हैं:
समतल और मुलायम चट्टानों की उपस्थिति।
विस्तृत कृषि उपजाऊ भूमि।
कम गहराई में जल की उपलब्धता—यह जल नदी या अन्य जल-स्रोतों से लिया जाता है, जो सिंचाई के लिए पर्याप्त होता है।
इन कारणों से इन राज्यों में इन सिंचाई साधनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है।
140. भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें।
उत्तर – भारतीय कृषि अनेक प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, और संरचना संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है। इन समस्याओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
1. प्राकृतिक समस्याएँ:
प्राकृतिक आपदाएँ (जैसे बाढ़ और सूखा)।
जल जमाव और परती तथा बंजर भूमि।
मिट्टी अपरदन और मिट्टी का अत्यधिक उपयोग।
2. आर्थिक समस्याएँ:
किसानों की निर्धनता।
अधिक उत्पादन लागत और कम उत्पाद मूल्य।
3. सामाजिक समस्याएँ:
कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का बोझ।
भूमि सुधार कार्यक्रमों का अप्रभावशाली कार्यान्वयन।
किसानों का तिरस्कार और उनके प्रति समाज की दृष्टि।
4. संरचना संबंधी समस्याएँ:
सिंचाई, उत्तम बीज, रासायनिक खाद, ऋण सुविधा, भंडारण और व्यवस्थित बाजार की कमी।

SANTU KUMAR
I am a passionate Teacher of Class 8th to 12th and cover all the Subjects of JAC and Bihar Board. I love creating content that helps all the Students. Follow me for more insights and knowledge.
Contact me On WhatsApp