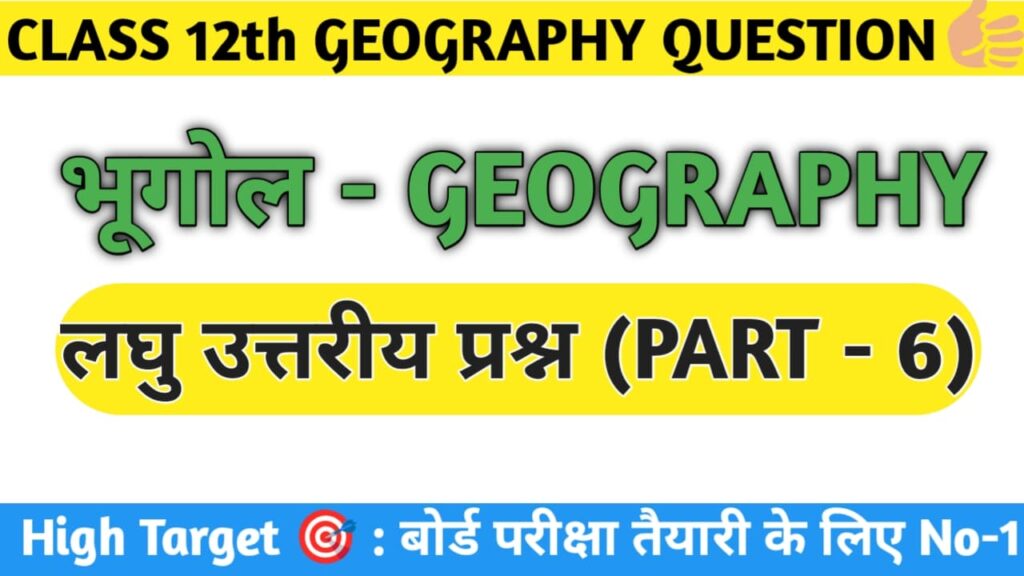100. जमशेदपुर एवं पुणे शहर के महत्त्व का उल्लेख करें।
उत्तर – जमशेदपुर
जमशेदपुर झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर बसा हुआ है और कोलकाता-मुंबई रेलमार्ग पर स्थित होने के कारण परिवहन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। यह क्षेत्र लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैंगनीज जैसे खनिजों से समृद्ध है, जिसके कारण यह भारत का एक प्रमुख लौह-इस्पात उद्योग केंद्र बन गया है।
यहाँ स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (टेल्को) जैसे उद्योगों ने जमशेदपुर को औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाया है। यहाँ लोहे-इस्पात के अलावा रेल इंजन, मध्यम और भारी वाहन आदि का भी निर्माण होता है।
पुणे
पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक नगर है। इसे ‘दस लाखी शहर’ के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का एक उभरता हुआ केंद्र है। इसके अलावा, यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, उच्च गुणवत्ता के साबुन और डिटर्जेंट जैसे उत्पादों का भी निर्माण होता है।
पुणे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। यहाँ पुणे विश्वविद्यालय के साथ-साथ कई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान हैं। साथ ही, यह फिल्म और कला के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है — यहाँ स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) देश भर में विख्यात है।
101. प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है ?
उत्तर – प्रदूषण
जब पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और इंसानों के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण के सभी घटकों की एक संतुलित संरचना होती है, लेकिन जब इसमें हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है।
प्रदूषण मुख्यतः मानव गतिविधियों जैसे कारखानों से निकलने वाले धुएँ, वाहनों से निकली गैस, खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, नालों का गंदा पानी, और कचरा आदि से होता है। हालांकि कुछ प्राकृतिक कारण भी प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और राख, बाढ़ का गाद और रेत आदि।
प्रदूषण के तीन मुख्य प्रकार हैं:
वायु प्रदूषण – हवा में हानिकारक गैसों का मिलना
जल प्रदूषण – नदियों, तालाबों आदि में गंदगी या रसायनों का पहुंचना
भूमि प्रदूषण – ज़मीन पर कचरे या रासायनिक पदार्थों का जमना
पर्यावरण में संतुलन बिगाड़ने वाले किसी भी हानिकारक तत्व को प्रदूषक कहा जाता है। ये तरल, ठोस या गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं, और हवा, पानी या ज़मीन के माध्यम से फैल सकते हैं।
102. जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए चार महत्त्वपूर्ण सुझाव दें।
उत्तर – जल प्रदूषण की रोकथाम के चार मुख्य सुझाव:
घरेलू कचरा जल स्रोतों में न डालें – घरों से निकले कचरे को नदियों, तालाबों या झीलों में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पानी गंदा होता है।
औद्योगिक अपशिष्टों का शुद्धिकरण जरूरी है – फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों और गंदे पानी को बिना साफ किए जल स्रोतों में नहीं छोड़ना चाहिए।
सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना – नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गंदा पानी साफ करने के लिए पर्याप्त और सही तरीके से काम करने वाले शोधन संयंत्र हों।
कड़े कानून और सख्त अमल – जल प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएँ और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए, ताकि दोषियों को सजा मिले और लोग सावधान रहें।
103. लोगों पर संदूषित जल/गंदे पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं ?
उत्तर – जल प्रदूषण और उसका प्रभाव
जल जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है। साफ और स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आज भारत के कई गाँवों और शहरों में जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जो एक गंभीर समस्या बन गई है।
जब जल के रंग, स्वाद, गंध या उसमें मौजूद तत्व इस तरह बदल जाते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और व्यापार के लिए नुकसानदायक हो, तो इसे जल प्रदूषण कहा जाता है।
प्रदूषित पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे—आँतों के रोग, पीलिया, हैजा, टायफायड, अतिसार और पेचिश आदि।
इसके अलावा, जब यह गंदा पानी खेतों में पहुँचता है, तो फसलों को भी नुकसान पहुँचता है। ऐसी फसलें जब भोजन के रूप में हमारे शरीर में जाती हैं, तो वे भी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं।
इसलिए, जल को स्वच्छ बनाए रखना न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
104. स्मॉग क्या होता है?
उत्तर – स्मॉग (धुंध और धुएँ का मिश्रण)
जब वायुमंडल में धुआँ और कुहासा मिलते हैं, तो उससे धुंआसा या स्मॉग बनता है। अंग्रेजी में इसे Smog कहा जाता है, जो Smoke (धुआँ) और Fog (कुहासा) से मिलकर बना है।
जाड़े के मौसम में अक्सर वातावरण की निचली सतह पर कुहासा बना रहता है। जब इस समय हवा में वाहनों, कारखानों और अन्य ईंधनों के जलने से निकला धुआँ मिल जाता है, तो स्मॉग का निर्माण होता है।
स्मॉग में मौजूद जहरीली गैसें और कण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। यह आँखों में जलन, सांस की तकलीफ, अस्थमा जैसी बीमारियाँ पैदा कर सकता है और खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।
105. हरित रासायनिकी क्या है ?
उत्तर – हरित रासायनिकी (Green Chemistry)
हरित रासायनिकी वह तरीका या सिद्धांत है, जिसके तहत रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ या बिल्कुल न पहुँचाएँ। इसका उद्देश्य हानिकारक रसायनों के निर्माण और उपयोग को कम करना या पूरी तरह रोकना होता है।
यह केवल रासायन बनाने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी रासायनिक उत्पाद के पूरा जीवन चक्र — उसके निर्माण, उपयोग और नष्ट करने तक — पर ध्यान देता है।
हरित रासायनिकी को कभी-कभी सतत् (सस्टेनेबल) रासायनिकी भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
प्रदूषण को पहले से ही रोकना,
मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना,
वातावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटाना,
और ऐसे रासायन तैयार करना जो कम हानिकारक हों।
इस प्रकार, हरित रासायनिकी एक पर्यावरण-मित्र और सुरक्षित रसायन निर्माण का मार्ग है।
106. मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं ?
उत्तर – वायु प्रदूषण और उसका प्रभाव
वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह खासतौर पर फेफड़ों, हृदय, स्नायु तंत्र (नर्वस सिस्टम) और परिसंचरण तंत्र (ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम) को प्रभावित करता है।
इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होता है, क्योंकि उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते और वे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं।
वायु प्रदूषण से केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समस्याएँ भी हो सकती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी आदि। इससे बच्चों और वयस्कों दोनों की सेहत और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है।
107. उष्माद्वीप क्या है? संक्षेप में लिखें।
उत्तर – उष्मा द्वीप (Heat Island)
शहरों के बीच के इलाकों में जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो वहाँ रहने और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े-बड़े सीमेंट और कंक्रीट के भवन बनाए जाते हैं। ये ढाँचे प्राकृतिक हरियाली को कम कर देते हैं और तापमान को बढ़ा देते हैं।
गर्मी के मौसम में इन इमारतों के कारण शहर का यह हिस्सा बहुत ज्यादा गरम हो जाता है, जिससे वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है।
ऐसे अत्यधिक गर्म शहरी क्षेत्र को “उष्मा द्वीप” या Heat Island कहा जाता है।
यह समस्या पर्यावरण असंतुलन और लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।
108. भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर – भारतीय नगरों में अपशिष्ट निपटान की समस्या
भारत के शहरों में अपशिष्टों (कचरे) के सही निपटान की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। इसके कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं:
सीवर की कमी – कई इलाकों में अभी भी मानव मल के निपटान के लिए पर्याप्त सीवर या अन्य सुरक्षित व्यवस्था नहीं है।
कचरा संग्रहण की असुविधा – ठोस कचरे (जैसे घरों का कूड़ा) को इकट्ठा करने और सही तरीके से निपटाने की सुविधा कमजोर है। इसके कारण सड़कों, खाली ज़मीनों और मोहल्लों में कचरे के ढेर लग जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।
औद्योगिक अपशिष्ट का जल प्रदूषण में योगदान – फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायनयुक्त गंदा पानी और अनुपचारित मलजल नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है और शहरों में गंभीर बीमारियाँ फैलती हैं।
हालाँकि सरकार और कुछ गैर-सरकारी संस्थाएँ इस दिशा में काम कर रही हैं, फिर भी यह समस्या अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। यदि इन अपशिष्टों को एक संसाधन के रूप में देखा जाए, तो इनसे ऊर्जा और जैविक खाद (compost) बनाई जा सकती है, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी होगी।
109. आप बस्ती (अधिवास) को कैसे परिभाषित करेंगे ?
उत्तर – मानव बस्ती या अधिवास
बस्ती या अधिवास उस स्थान को कहते हैं जहाँ लोग संगठित रूप से रहते हैं। इसमें उनके रहने के मकान, आने-जाने के रास्ते और गलियाँ शामिल होती हैं।
बस्तियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं — जैसे आखेटकों (शिकारियों) और चरवाहों के अस्थायी डेरे, स्थायी गाँव, और बड़े शहर। एक बस्ती कुछ घरों के छोटे से पुरवे (गाँव जैसे छोटे स्थान) से लेकर एक बड़े महानगर या मेगालोपोलिस तक हो सकती है।
लोगों का आवास भी भिन्न हो सकता है — यह एक झोपड़ी, साधारण मकान, फ्लैट, या फिर बड़ी हवेली के रूप में हो सकता है। इस प्रकार, मानव बस्तियाँ उसके रहन-सहन, आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार आकार और रूप में अलग-अलग हो सकती हैं।
110. स्थल या स्थान (साइट) एवं स्थिति (सिचुएसन) के मध्य अंतर बताएं।
उत्तर – स्थल और बस्ती की स्थिति
स्थल से तात्पर्य उस भूमि से है, जिस पर बस्ती स्थित होती है। यह स्थल किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे पहाड़ी इलाका, मैदानी क्षेत्र, नदी किनारा, या बाढ़ग्रस्त और बाढ़ रहित क्षेत्र। बस्ती का उदय या जनम उस स्थल पर निर्भर करता है, जहाँ वह बसी होती है।
बस्ती की स्थिति का मतलब है, बस्ती का स्थान उसके आस-पास के क्षेत्रों के मुकाबले कहाँ है। बस्ती कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापारिक क्षेत्र में से किसी भी एक में स्थित हो सकती है।
बस्ती की स्थिति, यानी उसका स्थान, उसके विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर बस्ती किसी उपजाऊ भूमि या व्यापारिक रास्ते पर स्थित होती है, तो उसका विकास तेज़ी से हो सकता है, जबकि कठिन परिस्थितियों में स्थित बस्तियाँ धीरे-धीरे विकसित होती हैं।
111. आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत करें।
उत्तर – नगरीय बस्तियाँ और उनका वर्गीकरण
नगरीय बस्तियाँ जनसंख्या के आकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बाँटी जाती हैं: शहर (Town), नगर (City), महानगर (Metropolis), और मेगानगर (Megacity)।
शहर (Town):
शहर वह बस्ती होती है जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो।
जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक हो।
75% पुरुष/श्रमिक गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हों।
शहर में नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या नगरीय क्षेत्र समिति होनी चाहिए।
नगर (City):
नगर वह बस्ती होती है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो।
महानगर (Metropolis):
महानगर वह बस्ती होती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो।
मेगानगर (Megacity):
मेगानगर वह बस्ती होती है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो।
इन श्रेणियों के आधार पर नगरीय बस्तियों का आकार और उनके विकास के तरीके अलग-अलग होते हैं। प्रत्येक श्रेणी की बस्तियों में आवश्यक सुविधाएँ और प्रशासनिक ढाँचा भी अलग होता है।
112. मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएँ।
उत्तर – मानव भूगोल और बस्तियों का अध्ययन
मानव भूगोल में मनुष्यों की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं को हम बस्तियों की संरचना और उनके कार्यों में साफ़ तौर पर देख सकते हैं।
बस्तियों का वर्तमान स्वरूप एक लंबे समय तक चले क्रमिक विकास का परिणाम है। प्राचीन समय में कृषि युग में ग्रामीण बस्तियाँ अधिक थीं, क्योंकि कृषि कार्य मुख्य रूप से गांवों में होते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद छोटे और बड़े सभी प्रकार की नगरीय बस्तियाँ उत्पन्न हुईं।
इसलिए, मानव भूगोल में बस्तियों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करता है, बल्कि यह बस्तियों के विकास और उनके परिवर्तनों को भी दर्शाता है।
113. बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं ?
उत्तर – बस्तियों का वर्गीकरण
बस्तियाँ आमतौर पर उनके आकार और कार्य के आधार पर ग्रामीण और नगरीय (या गाँव और नगर) दो श्रेणियों में बाँटी जाती हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच की सीमा पर विश्व में मतैक्य नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों में बस्तियों को ग्रामीण और नगरीय के रूप में पहचानने के लिए जनसंख्या की विभिन्न सीमा होती है।
उदाहरण के लिए:
जापान में 30,000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती ग्रामीण मानी जाती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में 2,500 से कम जनसंख्या वाली बस्ती ग्रामीण मानी जाती है।
कनाडा में 1,000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती ग्रामीण मानी जाती है।
भारत में 5,000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती ग्रामीण मानी जाती है।
ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से प्राथमिक कार्यकलाप (जैसे कृषि) होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में गैर-प्राथमिक कार्यकलाप (जैसे उद्योग, व्यापार) होते हैं।
इसके अलावा, ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, और इन्हें विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है:
जनसंख्या के आधार पर —
गाँव, शहर, नगर, महानगर, मेगालोपोलिस (मेगानगर)
आकृति के आधार पर —
संहत बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, रेखीय बस्ती, आयताकार बस्ती इत्यादि
कार्य के आधार पर —
प्राथमिक कार्य प्रधान बस्ती (जैसे गाँव)
प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, परिवहन, धार्मिक बस्तियाँ (जैसे नगर)
स्थिति के आधार पर —
मैदानी, पर्वतीय, पठारी, नदी तटीय, नदी के संगम, सड़क चौराहे इत्यादि पर स्थित बस्तियाँ
इस प्रकार, बस्तियों को उनके आकार, प्रकार, कार्य और स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
114. नगरीय बस्तियाँ किन रूपों में मिलती हैं ?
उत्तर – नगरीय बस्तियों की आकृतियाँ और उनका प्रभाव
नगरीय बस्तियाँ विभिन्न आकृतियों में होती हैं, जैसे रेखीय, वर्गाकार, तारा के समान या अर्द्ध चापाकार। नगर की आकृति उसकी स्थिति और भौगोलिक संरचना से प्रभावित होती है।
पहाड़ी क्षेत्रों पर बसे नगरों की आकृति सीढ़ीनुमा होती है।
नदी किनारे बसे नगर रेखीय (linear) होते हैं।
समतल मैदानी क्षेत्र के नगरों की आकृति वर्गाकार या आयताकार होती है।
नदी के संगम या समुद्री अन्तरीप पर बसे नगर त्रिभुजाकार होते हैं।
नगर की आकृति और वहाँ के भवनों की शैली उस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है।
इसके आधार पर नगरों को नियोजित और अनियोजित नगरों में बाँटा जा सकता है:
नियोजित नगर:
इन नगरों की आकृति सम होती है, और इनकी सड़कें और गलियाँ एक-दूसरे को समकोण (90°) पर काटती हैं।
उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ और जयपुर नियोजित नगर हैं।
अनियोजित नगर:
इन नगरों की आकृति विषम होती है और यहाँ की सड़कें, गलियाँ और मकान बेतरतीब तरीके से होते हैं।
115. ग्रामीण अधिवासों की पाँच विशेषताओं का उल्लेख करें।
उत्तर – ग्रामीण अधिवास की विशेषताएँ
ग्रामीण अधिवास की पाँच प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
आकार छोटा होता है:
ग्रामीण अधिवास का आकार सामान्यतः छोटा होता है। इस क्षेत्र में उतने ही लोग निवास कर सकते हैं, जितने लोगों का पालन-पोषण उस भूमि के संसाधनों और उत्पादन से संभव हो सकता है।
प्राथमिक गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं:
यहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, और मछली पकड़ना।
जनसंख्या घनत्व कम होता है:
ग्रामीण अधिवास में जनसंख्या का घनत्व नगरीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम रहता है।
मकानों का घनत्व कम रहता है:
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर मकानों का घनत्व भी कम होता है, यानी मकान एक-दूसरे से दूरी पर होते हैं।
आधुनिक सुविधाओं की कमी:
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़कें, शिक्षा संस्थान, और स्वास्थ्य सेवाएँ जैसी सुविधाओं की कमी होती है।
116. गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों के बीच अंतर कीजिए।
उत्तर – गच्छित (संहत) और प्रकीर्ण (बिखरी) बस्तियाँ
गच्छित (संहत) बस्तियाँ:
गच्छित बस्तियाँ वे होती हैं जिनमें मकान एक-दूसरे के समीप बनाए जाते हैं और यहाँ के निवासी मिलकर रहते हैं। इन बस्तियों में लोगों के व्यवसाय भी सामान्यतः समान होते हैं।
इस प्रकार की बस्तियाँ आमतौर पर नदी या घाटियों के उपजाऊ मैदानों में विकसित होती हैं।
प्रकीर्ण (बिखरी) बस्तियाँ:
प्रकीर्ण बस्तियाँ में मकान एक-दूसरे से दूर होते हैं और ये अक्सर खेतों द्वारा अलग होते हैं।
यह प्रकार की बस्तियाँ जंगली क्षेत्रों और पहाड़ी टीलों पर विकसित होती हैं।
117. भारत के चार बड़े राज्यों की जनसंख्या के आकार तथा क्षेत्रफल की तुलना कीजिए।
उत्तर – भारत में जनसंख्या का वितरण
भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भिन्नताएँ पाई जाती हैं। कुछ राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से बड़े हैं, कुछ राज्य क्षेत्रफल में बड़े हैं लेकिन उनकी जनसंख्या कम है, और कुछ राज्य क्षेत्रफल में छोटे हैं लेकिन उनकी जनसंख्या अधिक है।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े राज्य:
राजस्थान (10.41%)
मध्यप्रदेश (9.38%)
महाराष्ट्र (9.36%)
आन्ध्रप्रदेश (8.37%)
जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े राज्य:
उत्तरप्रदेश (16.17%)
महाराष्ट्र (9.42%)
बिहार (8.07%)
पश्चिम बंगाल (7.81%)
इस प्रकार, कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
राजस्थान और मध्यप्रदेश क्षेत्रफल में बड़े हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या कम है (राजस्थान: 5.57%, मध्यप्रदेश: 5.88%).
बिहार क्षेत्रफल में छोटा है (2.86%), लेकिन इसकी जनसंख्या अधिक है।
महाराष्ट्र क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में संतुलित और बड़ा राज्य है।
लगभग यही स्थिति आन्ध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश की भी है।
118. जन्मदर और मृत्युदर की प्रवृत्तियों ने भारत की जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार निर्धारित किया है ?
उत्तर – भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक
भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण कारक जन्मदर और मृत्युदर हैं।
1921 ई. से पहले दोनों दरें उच्च थीं। 1911-1921 में जन्मदर 48 प्रति हजार और मृत्युदर 47 प्रति हजार थी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी थी।
1921-1951 के बीच दोनों दरों में कमी आई, लेकिन मृत्युदर में ज्यादा कमी आई। 1941-1951 के बीच जन्मदर 40 प्रति हजार और मृत्युदर 27 प्रति हजार रही, जिससे जनसंख्या वृद्धि की गति तेज़ हुई।
1951-1981 के बीच भारत की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि जन्मदर में मामूली कमी (40 से 37 प्रति हजार) आई और मृत्युदर में बड़ी कमी (27 से 15 प्रति हजार) हुई।
1981 के बाद जन्मदर में और भी कमी आई, जिससे जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो गई।
भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर निम्नलिखित थी:
1911-21: 0.9 प्रति हजार
1941-51: 12.5 प्रति हजार
1971-81: 21 प्रति हजार
1991-1999: 17 प्रति हजार
119. संसार में जनसंख्या के आकार और घनत्व के संदर्भ में भारत के स्थान की विवेचना कीजिए।
उत्तर – भारत की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व
भारत की कुल जनसंख्या 102.8 करोड़ (2001) है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत है।
चीन के बाद, भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है।
हालांकि, भारत केवल 2.4 प्रतिशत विश्व के क्षेत्रफल पर स्थित है, और क्षेत्रफल में यह विश्व में सातवें स्थान पर है।
भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो चीन के औसत घनत्व (1997 में 129) से कहीं अधिक है।
संसार के दस सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भारत का स्थान बांग्लादेश (849) और जापान (334) के बाद तीसरा है।
120. भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेवार दो कारकों को लिखें।
उत्तर – भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए मुख्य रूप से प्राकृतिक स्वरूप और वर्षा का वितरण जिम्मेदार हैं।
प्राकृतिक स्वरूप में भिन्नता के कारण:
गंगा का मैदान और समुद्रतटीय मैदान जैसे उपजाऊ क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है और कृषि की स्थिति भी बेहतर रहती है।
इसके विपरीत, उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पठारी क्षेत्रों, साथ ही उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। यहाँ के स्थलाकृति और जलवायु के कारण कृषि और जीवन यापन की स्थितियाँ कठिन होती हैं।
वर्षा का वितरण:
उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा अधिक है, और वर्षा की यह मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है।
इस वर्षा की कमी के कारण पश्चिमी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी कम होता है।

SANTU KUMAR
I am a passionate Teacher of Class 8th to 12th and cover all the Subjects of JAC and Bihar Board. I love creating content that helps all the Students. Follow me for more insights and knowledge.
Contact me On WhatsApp