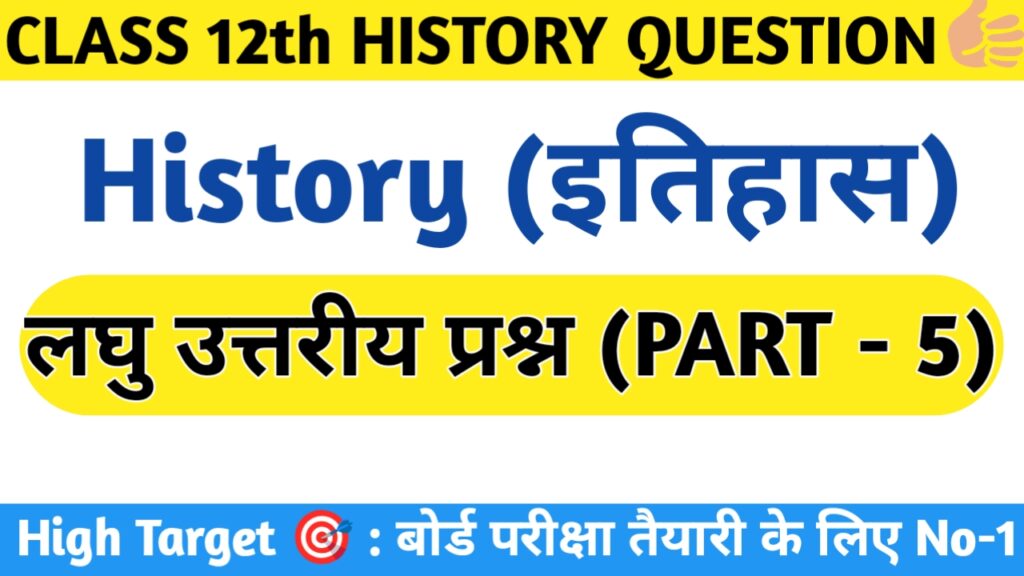Q.1. फोर्ट विलियम नामक किला कहाँ बनाया गया था ? बाद में यह जगह क्या हलाई ?
उत्तर – फोर्ट विलियम किला कोलकाता (कोल्कता) में बनाया गया था। यह किला 1696 में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। बाद में, इस किले के आसपास का इलाका शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो गया और यह क्षेत्र कोलकाता के केंद्रीय हिस्से में शामिल हो गया। फोर्ट विलियम का नाम बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम से जुड़ा। आजकल, यह किला भारतीय सेना के नियंत्रण में है और इसके आसपास के क्षेत्र को भी एक प्रमुख ऐतिहासिक और प्रशासनिक स्थल के रूप में जाना जाता है।
Q.2. ‘पाँचवीं रिपोर्ट’ पर टिप्पणी लिखें।
उत्तर – भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों से संबंधित यह पाँचवीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसे एक प्रवर समिति ने तैयार किया था, और यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इस रिपोर्ट में मुख्यत: जमींदारों, रैयतों की अर्जियाँ, कलक्टर की रिपोर्ट, और बंगाल-मद्रास के राजस्व के अलावा, न्यायिक अधिकारियों और उनके कार्यों पर टिप्पणियाँ की गई थीं। रिपोर्ट में जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, उनमें मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय जनता की समस्याएँ, प्रशासन की नीतियाँ और न्यायिक प्रणाली की कमियाँ शामिल थीं। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई, और इसने भारतीय प्रशासन के सुधार और ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएँ उत्पन्न कीं।
Q. 3. काँग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर – उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम और बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारतीय कांग्रेस में एक नए और तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के आदर्शों और तरीकों का आलोचक था। इस दल का प्रमुख उद्देश्य था कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य स्वराज (स्वतंत्रता) होना चाहिए। वे कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का विरोध करते थे और त्वरित और दृढ़ कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देते थे। 1905 से 1919 का काल भारतीय इतिहास में उग्रवादी युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय। उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का अपनाने पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना आवश्यक था। उग्रवादियों का यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
Q.4. स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गाँधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
उत्तर – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गांधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व रही है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उनका स्थान सर्वोच्च है, और भारत की स्वाधीनता का श्रेय मुख्य रूप से उनके योगदान को जाता है। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत की और जीवन के अंतिम क्षण तक देश सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन का पथ-प्रदर्शन करते रहे, यही कारण है कि उन्हें ‘राष्ट्रपिता’ के रूप में सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी शांति के दूत थे और उनके संघर्ष का आधार सत्य और अहिंसा था। उनका पूरा आंदोलन इन सिद्धांतों पर आधारित था। 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बावजूद, 1919 से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावशाली तरीके से प्रभावित करना शुरू किया और अंत तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्राण बने रहे। 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर पूरी तरह से गांधी जी के हाथों में रही। इस समय अवधि में उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के सर्वोच्च नेता के रूप में भारतीय राजनीति को मार्गदर्शन प्रदान किया, उसे नए विचार दिए, उसे सक्रिय किया और उसे जन-आंदोलन का रूप दिया। इसी कारण इस अवधि को ‘गांधी युग’ के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी नीतियों और नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया दिशा और उद्देश्य दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता का सपना साकार हो सका।
Q. 5. गाँधीजी 1917 में चम्पारण क्यों गये? वहाँ उन्होंने क्या किया?
उत्तर – 19वीं सदी के प्रारम्भ में गोरे बागान मालिकों ने भारतीय किसानों के साथ एक अनुबंध किया, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस पद्धति को ‘तिनकठिया’ पद्धति कहा जाता था। इस अनुबंध के तहत किसान नील की खेती के लिए मजबूर थे, जो उनकी जीवन-यात्रा के लिए कठिनाइयों और शोषण का कारण बनता था। किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। 1917 में चम्पारण के एक प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से संपर्क किया और उनके मार्गदर्शन में चम्पारण के किसानों की पीड़ा को उजागर करने का अनुरोध किया। गांधी जी ने उनकी अपील स्वीकार की और चम्पारण पहुंचे। गांधी जी के नेतृत्व में किसान संघर्ष तेज़ हुआ और उनकी मांगों को लेकर जनता में जागरूकता फैलनी शुरू हुई। गांधी जी के प्रयासों के परिणामस्वरूप, सरकार ने चम्पारण के किसानों की समस्याओं की जाँच हेतु एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के समक्ष गांधी जी ने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। अंततः गांधी जी की विजय हुई और चम्पारण के किसानों को राहत मिली। इस संघर्ष की सफलता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और यह गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के रूप में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
Q.6.औद्योगिक शहर के रूप में ब्रिटिश काल में किन नगरों का उदय हआ ?
उत्तर – ब्रिटिश काल में भारत में औद्योगिक विकास बहुत सीमित था और केवल दो नगरों में ही औद्योगिक गतिविधियाँ प्रमुख रूप से विकसित हुईं। पहला नगर था कानपुर, जहाँ मुख्य रूप से सूती कपड़े, ऊनी कपड़े और चमड़े की वस्तुएं का उत्पादन होता था। कानपुर उस समय भारतीय कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ का उत्पादन ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करता था। दूसरा नगर था जमशेदपुर, जहाँ स्टील का उत्पादन होता था। जमशेदपुर ने भारतीय धातु उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यहाँ की स्टील मिल्स ने भारतीय उद्योग की नींव रखी। हालाँकि, ब्रिटिश काल में भारत में अन्य औद्योगिक नगरी का विकास नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश शासन की पक्षपाती नीति, जो औद्योगिक विकास को सीमित रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि वे एक औपनिवेशिक देश की भूमिका में भारत को रखते हुए उसकी आर्थिक वृद्धि को अवरुद्ध करें, ताकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक कच्चे माल का स्रोत और तैयार उत्पादों का बाजार बना रहे। इसलिए, भारत में औद्योगिकीकरण का विकास बहुत धीमा था और केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित था।
Q.7. अमरीको गृहयुद्ध और स्वेज नहर का प्रारम्भ होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?
उत्तर – अमेरिका में गृहयुद्ध का प्रारंभ 1861 में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका से कपास का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंद हो गया। इसके कारण, भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई, क्योंकि अब तक अमेरिकी कपास का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। भारत में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होता था। इस अवसर का फायदा भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों ने उठाया, जिन्होंने कपास के व्यापार में अच्छा लाभ कमाया। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ, जिससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग बहुत छोटा और तेज हो गया। इसके साथ ही बम्बई शहर का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। स्वेज नहर के माध्यम से बम्बई से अन्य देशों के साथ व्यापार करना बहुत आसान हो गया। बम्बई के कपड़ा उद्योग में भारी निवेश हुआ और इसके कारण बम्बई भारत का सबसे अधिक व्यस्त और व्यापारिक केंद्र बन गया। इस समय बम्बई न केवल कपड़ा उद्योग बल्कि पूरे भारतीय व्यापार का प्रमुख हब बन गया।
Q.8. राष्ट्रवादियों तथा साम्प्रदायवादियों में मुख्य अन्तर क्या था ?
उत्तर – राष्ट्रवादी भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखते थे, जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर, सम्मानपूर्वक और शांति से रहते थे। उनका विश्वास था कि भारत एकता, विविधता और सहअस्तित्व का प्रतीक होना चाहिए। दूसरी ओर, साम्प्रदायिकतावादी भारत को धर्म के आधार पर विभाजित समूहों के रूप में देखते थे। वे व्यक्तिगत और धार्मिक हितों को राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व देते थे। इसी दृष्टिकोण को आधार बनाकर ही मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की माँग की गई थी। उनका मानना था कि मुसलमानों का धर्म और संस्कृति हिन्दू बहुल समाज से अलग है, और इसलिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से मुसलमानों के हितों और पहचान को सुरक्षित रख सके। यह सोच और दृष्टिकोण बाद में पाकिस्तान के निर्माण का कारण बनी।
Q.9. संविधान निर्माताओं की प्रमुख समस्याएँ क्या थी ?
उत्तर – भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए संविधान बनाना कोई सरल कार्य नहीं था। संविधान निर्माताओं के सामने कई प्रमुख समस्याएँ थीं, जिन्हें हल करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। ये समस्याएँ निम्नलिखित थीं:
भारत की अखंडता को बनाए रखना – भारत की विविधता और विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश की अखंडता को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। संविधान निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना था कि सभी प्रांतों और क्षेत्रों के बीच संतुलन बना रहे और देश एकजुट रहे।
देशी रियासतों की समस्या – देशी रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने या नहीं होने की स्थिति भी एक बड़ी समस्या थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्रस्ताव में इन रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने या न होने की छूट दी थी, जिससे यह सुनिश्चित करना कठिन था कि सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हों और भारत की एकता बनाए रखी जाए।
भारत की सांस्कृतिक विविधता – भारत में विभिन्न जातियाँ, जनजातियाँ, और भाषाएँ हैं, और सभी के हितों को एक संविधान में समाहित करना एक बड़ी चुनौती थी। आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें न्याय प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी।
अंग्रेजी शासनकाल की शोषण और उत्पीड़न की धरोहर – अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में व्यापक शोषण और उत्पीड़न हुआ था, और स्वतंत्रता के साथ आम भारतीयों की कई आशाएँ जुड़ी हुई थीं। संविधान निर्माताओं को इन आशाओं को पूरा करते हुए एक नया और न्यायपूर्ण भारत बनाना था, ताकि भारतीय नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकें और उन्हें बेहतर जीवन की उम्मीद हो।
इन सभी समस्याओं के बावजूद, संविधान निर्माताओं ने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि से भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया, जो न केवल देश की विविधता को सम्मानित करता है, बल्कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ।
Q.10. 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करें –
उत्तर – 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण:
1857 का विद्रोह भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक विशाल और संघर्षपूर्ण प्रयास था। इस विद्रोह ने भारतीयों में स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को जागृत किया, लेकिन कुछ कारणों के कारण यह विद्रोह असफल रहा। इस असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:
विद्रोह की तिथि में असमंजस – इस विद्रोह की शुरुआत के लिए एक निश्चित तिथि, 31 मई 1857, निर्धारित की गई थी, लेकिन यह 10 मई 1857 को अचानक शुरू हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्रोहियों के बीच सामूहिक एकजुटता और समन्वय की कमी हो गई, जिससे उन्हें अंग्रेजों का सामना करना मुश्किल हो गया।
व्यापक फैलाव और संचार का अभाव – यह स्वतंत्रता संग्राम पूरे भारत में फैलने की बजाय कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। परिवहन और संचार के अभाव के कारण भारतीय सेनापतियों और विद्रोहियों के लिए सभी क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रण रखना संभव नहीं हो पाया। इससे समन्वय की कमी रही और विद्रोह को अधिक व्यापक रूप से फैलने में कठिनाई हुई।
हथियारों का अभाव – भारतीय सैनिकों और विद्रोहियों के पास अंग्रेजों के मुकाबले अत्याधुनिक हथियारों का अभाव था। अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य साजो-सामान और हथियार थे, जिससे उन्हें विद्रोहियों के मुकाबले सैन्य लाभ मिला।
कुछ वर्गों का असक्रिय रहना – भारत के कुछ सामाजिक और धार्मिक वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। विशेषकर, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी मतभेद, साथ ही अन्य जातीय और सांप्रदायिक तनावों के कारण कई वर्ग इस संघर्ष से बाहर रहे, जो विद्रोह को कमजोर बनाता था।
कुशल सेनापतियों का अभाव – भारतीयों के पास अंग्रेजों के समान कुशल सेनापतियों और रणनीतिक नेताओं की कमी थी। अंग्रेजों के पास अनुभवी और प्रशिक्षित कमांडर थे, जिन्होंने विद्रोहियों का समाना किया और उन्हें रणनीतिक रूप से हराया।
ब्रिटेन से समय पर सहायता – अंग्रेजों को ब्रिटेन से यथासमय सैन्य और संसाधनों की सहायता प्राप्त होती गई, जिससे उन्हें युद्ध में लगातार समर्थन मिलता रहा और वे भारतीयों पर काबू पा सके।
योजना और उद्देश्यों की कमी – विद्रोहियों में एक ठोस और सुसंगत योजना एवं उद्देश्य की कमी थी। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विद्रोह हो रहे थे, लेकिन उनमें कोई केंद्रीय नेतृत्व या उद्देश्य नहीं था, जिससे विद्रोह को संगठित और प्रभावी तरीके से चलाना संभव नहीं हो पाया।
इन कारणों से 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे आने वाले वर्षों में भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के लिए प्रेरित किया।
Q.11. शैलावासों की स्थापना के प्रमुख कारण क्या थे ? अथवा, ब्रिटिश शासकों के लिए हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण थे ?
उत्तर – शैलावास, जिन्हें अंग्रेजी में ‘हिल स्टेशन’ कहा जाता है, प्रमुखतः स्वास्थ्यवर्धक स्थलों के रूप में स्थापित किए गए थे। इन हिल स्टेशनों का उद्देश्य खासतौर पर उन स्थानों पर जाने वाले लोगों को ठंडी और ताजगी प्रदान करना था, जहाँ वे गर्मी, बीमारी या अन्य कारणों से राहत पा सकें। भारत के प्रायः सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे हिल स्टेशनों की स्थापना की गई है। इन हिल स्टेशनों की स्थापना का एक प्रमुख कारण स्वास्थ्य लाभ और पर्यटन को बढ़ावा देना था। लोग विशेषकर इन स्थलों पर शांति, ताजगी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए जाते हैं। इसके अलावा, हिल स्टेशनों की स्थापना का एक अन्य कारण पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बनाना भी था। भारत में विभिन्न हिल स्टेशनों का विकास हुआ है, जैसे राजस्थान में माउंट आबू, दक्षिण भारत में ऊटी, उत्तर भारत में मसूरी, और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी प्रमुख हिल स्टेशनों के रूप में विकसित हुए हैं। इसके अलावा, भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य भी मुख्य रूप से हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध हैं और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अंग्रेजों के लिए इन हिल स्टेशनों की स्थापना का एक और कारण था कि वे गर्म जलवायु के आदी नहीं थे। इसलिए, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने इन हिल स्टेशनों का निर्माण किया, ताकि वे गर्मी से बचने के लिए वहाँ रह सकें। इन हिल स्टेशनों ने न केवल अंग्रेजों को राहत प्रदान की, बल्कि भारतीयों के लिए भी स्वास्थ्य और पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल बन गए।
Q.12. मंगल पांडे कौन थे ? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए।
उत्तर – मंगल पांडे भारतीय इतिहास में एक प्रमुख क्रांतिकारी और महान देशभक्त के रूप में विख्यात हैं। उन्हें 1857 के विद्रोह का प्रथम जनक माना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया साहसिक कदम इस विद्रोह की जड़ें जमाने में सहायक सिद्ध हुआ। मंगल पांडे बैरकपुर (बंगाल) की 34वीं सैन्य बटालियन के एक साधारण सिपाही थे। उन्होंने अपने छावनी में अंग्रेजों द्वारा वितरित चर्बी वाले कारतूस के बारे में सैनिकों के बीच जानकारी फैलाई, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों दोनों के लिए धर्म विरोधी थे। इस कारतूस के बारे में उनकी अवहेलना ने अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी को जन्म दिया। जब सार्जेंट मेजर हगसन के आदेश पर पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कोई भारतीय सैनिक आगे नहीं आया, तो पांडे ने हगसन और लैफ्टिनेंट बाम को उनके घोड़े सहित मार डाला। इसके बाद पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फाँसी दे दी गई। मंगल पांडे की वीरता और कुर्बानी ने भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना को उत्तेजित किया और इसने मेरठ सैनिक छावनी में होने वाले विद्रोह की दिशा तैयार की। उनका साहस और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।
Q. 13. नाना साहिब कौन थे ? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए।
उत्तर – नाना साहिब, जो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नाना साहिब को अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में विद्रोह छेड़ने के लिए विद्रोहियों द्वारा उकसाया गया था। जब कानपुर के सिपाहियों और शहरवासियों ने नाना साहिब के समक्ष बगावत की बागडोर संभालने की प्रार्थना की, तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, और उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहिब को न तो पेशवा माना और न ही उन्हें पेंशन दी। इस स्थिति में नाना साहिब का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा उनके अधिकारों को नकारे जाने और अपमानित करने के बावजूद, नाना साहिब ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अंग्रेजों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया, तो नाना साहिब ने तात्या टोपे की मदद से अंग्रेज सेनापति नील और हैवलॉक को पराजित किया और कानपुर के किले पर पुनः कब्जा कर लिया। यह एक बड़ा सैन्य संघर्ष था, जिसमें नाना साहिब की रणनीति और साहस को सराहा गया। हालांकि, दिसम्बर 1857 में, जब नई अंग्रेजी सेना आयी, तो सर कोलिन कैम्पवेल ने नाना साहिब को पराजित कर लिया। नाना साहिब हालांकि अंग्रेजों के हाथों नहीं आए। वे नेपाल की ओर भागने में सफल रहे। नाना साहिब की यह कूटनीतिक चाल उनके साहस और बहादुरी का प्रतीक मानी जाती है। उनके प्रशंसक उन्हें एक साहसी और रणनीतिक नेता के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया।
Q.14. तात्या टोपे कौन था ? उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए।
उत्तर – तात्या टोपे नाना साहिब की सेना के एक अत्यंत कुशल, साहसी, परमवीर और विश्वसनीय सेनापति थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने अद्वितीय सैन्य कौशल और रणनीति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तात्या टोपे ने कानपुर में गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाते हुए अंग्रेजों की सेना को कठिन संघर्ष में डाल दिया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उनकी युद्ध रणनीति ने अंग्रेजों के लिए कई समस्याएँ उत्पन्न कीं, और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक बन गए। तात्या टोपे ने अंग्रेज जनरल बिन्द्रहम को बुरी तरह परास्त किया, जो उनकी युद्ध कला और रणनीतिक कौशल का प्रमाण था। इसके अलावा, उन्होंने झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर झाँसी की रक्षा में उनका पूर्ण निष्ठा से सहयोग किया, और इस दौरान उन्होंने वीरता और साहस की मिसाल पेश की। हालांकि, तात्या टोपे की यह संघर्षपूर्ण यात्रा अंततः असफल रही। सर कोलिन कैम्पवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने उन्हें हराया। 1858 में, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी की सजा दी, लेकिन उनकी बहादुरी और संघर्ष को हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में याद किया जाएगा। तात्या टोपे को न केवल एक महान सेनापति के रूप में, बल्कि एक साहसी और निष्ठावान नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है।
Q. 15. लक्ष्मीबाई कौन थी ? संक्षिप्त परिचय दीजिए।
उत्तर – रानी लक्ष्मीबाई झाँसी (उत्तर प्रदेश) की वीरता और साहस का प्रतीक थीं। जब उन्हें संतान नहीं हुई, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लेकर उसे झाँसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि, अंग्रेजों ने रानी के इस उत्तराधिकार के अधिकार को मान्यता नहीं दी, जिसके कारण वह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो गईं। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष किया और नाना साहिब के विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित किया। उनका यह साहसिक कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंत में, रानी लक्ष्मीबाई कालपी के स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी बहादुरी और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हैं और उनका संघर्ष सभी के लिए एक प्रेरणा बना। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और निडरता आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित है।
Q.16. 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे ?
उत्तर – 1857 के सिपाही विद्रोह के महत्त्वपूर्ण प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:
सामाजिक कारण (Social causes) – अंग्रेजों ने भारतीय समाज में कई सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया और विधवा पुनर्विवाह की कानूनी अनुमति दी। इसके साथ ही स्त्रियों को शिक्षा देने का काम भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने रेलवे और अन्य यातायात के साधनों को बढ़ावा दिया। हालांकि, रूढ़िवादी भारतीय इन सभी सुधारों को संदेह की दृष्टि से देखते थे और उन्हें यह भय था कि अंग्रेज हमारे पारंपरिक समाज और धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करना चाहते हैं।
धार्मिक कारण (Religious causes) – अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत में धर्म परिवर्तन कराने का स्वतंत्रता दी। इसके अलावा, अंग्रेजों ने मंदिरों और मस्जिदों की ज़मीन पर कर लगा दिया, जिससे पंडितों और मौलवियों में गहरी नाराजगी फैल गई। इस असंतोष के कारण, उन्होंने जनता में अंग्रेजों के खिलाफ जागृति फैलानी शुरू की, जिससे विद्रोह को हवा मिली।
सैनिक कारण (Military causes) – भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच पद, वेतन और पदोन्नति के मामलों में भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता और उन्हें हमेशा कम महत्त्व दिया जाता था। इसके अलावा, सामूहिक रसोई होने के कारण उच्च वर्ग के ब्राह्मण और ठाकुर लोग निम्न वर्ग के सैनिकों के साथ खाना खाने से परहेज़ करते थे, जिससे सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया।
तात्कालिक कारण (Immediate causes) – कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल था, जिसे लेकर विद्रोह भड़क उठा। नयी स्वफील्ड बंदूकों में गोली भरने से पहले कारतूस को दाँत से छीलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में गाय और सूअर को अपवित्र माना जाता था। ऐसे में इस चर्बी का प्रयोग उनके धर्म के खिलाफ था, जिससे सैनिकों का गुस्सा स्वाभाविक रूप से बढ़ा और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया।
इन सभी कारणों ने मिलकर 1857 के सिपाही विद्रोह को जन्म दिया, जो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
Q.17. 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था ?
उत्तर – 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण कारतूसों में लगी सूअर और गाय की चर्बी थी। नई स्वफील्ड बंदूकों में गोली भरने से पहले कारतूस को दाँत से छीलना पड़ता था, और इन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। यह दोनों चीजें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक दृष्टि से अपवित्र मानी जाती थीं। इसलिए, इन कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म के खिलाफ था, जिससे सिपाही भड़क गए। 26 फरवरी, 1857 को बहरामपुर में 19वीं नेटिव एनफैंट्री के सिपाहियों ने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसके बाद, 19 मार्च, 1857 को चौंतीसवीं नेटिव एनफैंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बाद में, उन्हें पकड़कर फाँसी दे दी गई। इस प्रकार, सिपाहियों का निर्णायक विद्रोह 10 मई, 1857 को मेरठ में शुरू हुआ, जिससे 1857 का सिपाही विद्रोह पूरे देश में फैल गया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया।
Q.18. ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा ?
उत्तर – ब्रिटिश पत्र-पत्रिकाओं, अखबारों और कार्टूनों में 1857 के विद्रोह के दो प्रमुख बिन्दुओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। पहले, हिंदुस्तानी सिपाहियों की बर्बरता और दूसरे, ब्रिटिश सत्ता की अजेयता का प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में, टॉमस जोन्स वर्कर के 1859 में प्रकाशित चित्र “रिलीज ऑफ लखनऊ इन मेमोरियम” और “न्याय” जैसे चित्रों के माध्यम से ब्रिटिशों ने अपनी प्रतिरोध की भावना और अजेयता को दर्शाया। इन चित्रों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिरोध को तो न्यायपूर्ण और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया गया, वहीं भारतीय विद्रोहियों को बर्बर और हिंसक रूप में चित्रित किया गया। ब्रिटिश मीडिया ने इस विद्रोह को अपनी विजय और शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, जो उनकी साम्राज्यवादी मानसिकता को दर्शाता है।

SANTU KUMAR
I am a passionate Teacher of Class 8th to 12th and cover all the Subjects of JAC and Bihar Board. I love creating content that helps all the Students. Follow me for more insights and knowledge.
Contact me On WhatsApp