Q.1. रैयतवाडी व्यवस्था क्या थी? इससे क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हए ?
उत्तर – दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके तहत किसान भूमि का मालिक था, बशर्ते वह भू-राजस्व का नियमित भुगतान करता रहे। इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना था कि यह वही व्यवस्था है, जो भारत में पहले लागू थी। बाद में यह व्यवस्था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 20-30 वर्ष बाद संशोधन कर राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। हालांकि, इस व्यवस्था में कुछ प्रमुख त्रुटियाँ थीं:
(i) भू-राजस्व 45 से 55 प्रतिशत था, जो बहुत अधिक था और किसानों पर भारी बोझ डालता था।
(ii) भू-राजस्व बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था, जिससे किसानों पर सरकारी दबाव बढ़ गया।
(iii) सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद किसानों को पूरा राजस्व देना पड़ता था, जिससे किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई और भूमि पर उनका प्रभुत्व कमजोर पड़ गया।
प्रभाव –
(i) इस व्यवस्था के कारण समाज में असंतोष और आर्थिक विषमता का वातावरण फैल गया।
(ii) सरकारी कर्मचारी किसानों पर अत्याचार करते रहे, और किसानों का शोषण पहले जैसा ही जारी रहा।
इस प्रकार, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बावजूद किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, और यह व्यवस्था समाज में असंतोष का कारण बनी।
Q.2. महालबाडी व्यवस्था क्या थी ?
उत्तर – महालबाड़ी नामक भू-व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था (स्थायी व्यवस्था) का ही एक संशोधित रूप थी। यह व्यवस्था 1801 ई. में अवध क्षेत्र और 1803-04 में मराठे अधिकृत प्रदेशों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रति खेत के आधार पर लगान नहीं तय किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल (गाँव या जागीर) के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था में पूरा गाँव मिलकर लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी था। महालबाड़ी व्यवस्था में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था, बल्कि समस्त गाँव का स्वामित्व था। इसलिए इसे महालबाड़ी व्यवस्था कहा गया, क्योंकि गाँव के सामूहिक रूप से लगान देने और भूमि पर सामूहिक अधिकार को इस व्यवस्था के तहत लागू किया गया था।
Q.3. स्थायी बंदोबस्त से कम्पनी को हुए लाभों का वर्णन करें।
उत्तर – स्थायी व्यवस्था से पूर्व राज्य की आय निश्चित नहीं थी। उच्चतम बोली देने वाले बहुत कम जमींदार समय पर अपनी धनराशि की अदायगी कर पाते थे, जिससे सरकार की आय अनिश्चित बनी रहती थी। स्थायी व्यवस्था के लागू होने के बाद, सरकार को जमींदारी से प्राप्त धन का एक निश्चित भाग मिलने लगा। यदि कोई जमींदार समय पर धन की अदायगी नहीं कर पाता था, तो उसकी भूमि क़ब्ज़ा कर ली जाती थी। क्योंकि भू-राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, इसलिए सरकार ने कम्पन के योग्य कर्मचारियों को इस राजस्व को वसूल करने के लिए नियुक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे विभागों का कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा था। हालांकि, इस व्यवस्था के कारण सरकार को निश्चित आय प्राप्त हुई और सरकार ने अन्य योग्य व्यक्तियों को अन्य विभागों में नियुक्त करना शुरू किया, जिससे शासन व्यवस्था की क्षमता बढ़ी और शासन संचालन में सुधार हुआ।
Q.4. मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
उत्तर – अकबर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनसबदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इस व्यवस्था में मनसबदार को दो पद—जात और सवार—प्रदान किए जाते थे। ब्लाकमैन के अनुसार, जात एक मनसबदार को जितने सैनिक रखने पड़ते थे, उसका सूचक था, जबकि सवार उस संख्या को दर्शाता था, जितने घुड़सवार सैनिक मनसबदार के पास होते थे।
मनसबदारी व्यवस्था के तहत:
- 40 से 500 तक का मनसबदार मनसबदार कहलाता था।
- 500 से 2500 तक का मनसबदार अमीर कहलाता था।
- 2500 से अधिक का मनसबदार अमीर-ए-उम्दा कहलाता था।
मनसबदारों को वेतन के रूप में नकद रकम मिलती थी, और कभी-कभी उन्हें जागीर भी दी जाती थी। इस प्रकार, मनसबदारी व्यवस्था मुग़ल सेना का प्रमुख आधार बन गई और अकबर के साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Q.5. मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर – मीराबाई (1498-1547) भक्ति साहित्य की प्रमुख कवियित्रियों में से एक थीं, जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुईं। उनका जीवन एक संघर्ष और प्रेम का प्रतीक था। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमे रहने वाली एक महान संत और कवयित्री थीं। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह से हुआ था, लेकिन वे विवाह के बंधन में बंधकर भी समाज के पारंपरिक नियमों से बाहर अपनी भक्ति और आत्मिक स्वतंत्रता का पालन करती रही। उनकी काव्य रचनाएँ भक्तिकाव्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं, जिसमें उनके गीतों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी प्रेमभावना और उनके साथ आत्मसात होने की इच्छा व्यक्त की गई है। मीराबाई की रचनाएँ हिंदी भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं और उनके पदों में प्रेम, समर्पण और आत्मसमर्पण की भावना प्रकट होती है। वे भारतीय समाज के विभिन्न कठोर परंपराओं, विशेषकर स्त्री-रहन-सहन और सामाजिक बंधनों को नकारते हुए अपने व्यक्तिगत भक्ति मार्ग पर चलीं, जिससे उनकी पूजा और भक्ति के प्रति उनकी अविचल निष्ठा समाज में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। मीराबाई को उनके अनन्य कृष्ण भक्ति के कारण आज भी भक्ति आन्दोलन की प्रेरणास्त्रोत के रूप में याद किया जाता है।
Q.6. सन्त नामदेव पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर – संत नामदेव (1270-1350) भारतीय भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक थे, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और पंजाब क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था, और वे एक समर्पित भक्त थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित किया। उनका योगदान सिख धर्म में भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपने भक्ति गीतों और पदों के माध्यम से सिखों के गुरुओं को प्रभावित किया। नामदेव की भक्ति केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि उनके जीवन का सच्चा अर्थ और उद्देश्य था। वे निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, जिसका अर्थ था कि ईश्वर के कोई रूप नहीं होते और वह सर्वव्यापी हैं। उन्होंने न केवल भगवान की पूजा की, बल्कि समाज के सभी वर्गों को धर्म के प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया। वे सामाजिक विषमताओं और पाखंड के खिलाफ थे और उनके भक्ति पदों में मानवता, समानता और एकता का संदेश मिलता है। नामदेव के भक्ति गीत और पद आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका काव्य साहित्य और भजन सरल, सीधे और भावनात्मक थे, जो सीधे मन को छूते थे। उनके पदों का प्रभाव भारतीय भक्ति साहित्य पर गहरा था और वे सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक के भी प्रेरणास्त्रोत बने। नामदेव की शिक्षा और उनका जीवन दर्शन यह संदेश देता है कि भक्ति में केवल संप्रदाय का नहीं, बल्कि सार्वभौमिक प्रेम और समर्पण का स्थान है। उनका योगदान भक्ति आंदोलन के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, और उन्हें भारतीय संतों की परंपरा में एक आदर्श के रूप में याद किया जाता है।
Q.7. कबीर पर एक टिप्पणी लिखिए।
उत्तर – कबीर (1440-1518) भारतीय संत और कवि थे, जो भक्ति आंदोलन के महान संत माने जाते हैं। वे एक महान निर्गुण भक्त थे, और उनके काव्य में भगवान के निराकार रूप की पूजा का संदेश प्रमुखता से मिलता है। कबीर का जीवन और दर्शन सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक था। उनका जन्म वाराणसी के पास हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन में संप्रदाय, जाति और धर्म के बंधनों को नकारते हुए एक नया मार्ग दिखाया। कबीर के गीतों और कविताओं में सच्चे प्रेम, आध्यात्मिक जागृति, और धार्मिक एकता की गहरी भावना है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के पाखंड और बाहरी आडंबरों की आलोचना की, और केवल एकता और प्रेम की बात की। कबीर के अनुसार, भगवान का असली रूप निराकार है, और वह सबमें व्याप्त है। उनका प्रसिद्ध मंत्र “हामी न हिंदू, न मुसलमान” इस बात का प्रतीक था कि धार्मिक भेदभाव से परे एक सच्चा भक्त वही है, जो ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को सर्वत्र अनुभव करता है। कबीर की वाणी सीधे, सरल और प्रभावी थी, जो हर वर्ग के लोगों को समझ में आती थी। उनकी बीजक और कबीर वाणी में जीवन की सच्चाई, प्रेम और समर्पण का गहरा संदेश छिपा हुआ है। उनके भजन और कविताएँ आज भी जनमानस में लोकप्रिय हैं और उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक एकता की नींव रखी। कबीर का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें धार्मिक भेदभाव को छोड़कर मानवता, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर मार्गदर्शन करता है। वे एक युग परिवर्तनक समाज सुधारक थे, और उनकी वाणी आज भी सत्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में हमारे बीच जीवित है।
Q.8. रामानुज और रामानंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर – रामानुज (1017-1137) भारतीय संत और वैष्णव आचार्य थे, जिन्हें विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रणेता माना जाता है। वे श्री विष्णु के परम भक्त थे और उनका दर्शन वेदांत के अद्वैत सिद्धांत से भिन्न था। रामानुज ने यह माना कि ब्रह्म एक है, लेकिन उसमें साकार और निर्गुण दोनों रूपों में ईश्वर की उपासना की जा सकती है। उनका मानना था कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद सच्चा है, और मानवता के उद्धार के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। रामानुज के सिद्धांतों ने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी और वे श्री विष्णु की पूजा के लिए एक संगठित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। वे तमिलनाडु में शृंगेरी मठ के प्रमुख आचार्य बने और उन्होंने अध्वैतवाद के स्थान पर विष्णु भक्तिवाद की स्थापना की। उनके अनुयायी रामानुज समाज के रूप में प्रसिद्द हुए और उनका योगदान भारतीय धार्मिक और भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण है।रामानंद (14वीं सदी) एक महान संत और भक्ति आंदोलन के प्रर्वतक थे। वे प्रमुख रूप से राम भक्ति के सिद्धांतों के प्रचारक थे और राम के प्रति भक्ति को अत्यधिक महत्व देते थे। रामानंद ने भक्ति मार्ग को सरल और सुलभ बनाया, जिससे यह समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर नीच जातियों और दलितों के लिए खुला। उन्होंने जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ते हुए भक्ति का संदेश दिया कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, या वर्ग से हो, ईश्वर की भक्ति में समान रूप से भागीदार हो सकता है। उनका यह सिद्धांत कि राम का नाम ही सर्वोत्तम है, भारतीय समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने में सफल रहा। रामानंद के अनुयायी राम-नाम की महिमा का प्रचार करने में संलग्न थे और उनके मार्गदर्शन में भक्तिमार्ग का प्रचार हुआ। रामानंद की भक्ति और दर्शन ने भारतीय समाज में एक नया अध्याय जोड़ा और उन्होंने राम भक्तों की एक बड़ी धारा का निर्माण किया।
Q.9. गुरु नानक कौन थे ? उनके व्यक्तित्व के बारे में किसी एक इतिहासकार का कथन लिखिए।
उत्तर – गुरु नानक (1469-1539) सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। वे एक महान संत, शिक्षक और समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म, भक्ति, और समानता का संदेश दिया। उनका जीवन और दर्शन धर्म और जातिवाद की बेड़ियों से परे था। उन्होंने ईश्वर के एकत्व और मानवता की महत्वपूर्ण बातें उठाईं और सभी धर्मों के अनुयायियों को मानवता और प्यार की दिशा में एकजुट होने का संदेश दिया। गुरु नानक ने अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और न्याय की नींव पर खड़ा किया और उन्होंने यह सिखाया कि सत्य, सेवा, और ईश्वर के प्रति निष्ठा ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। गुरु नानक ने “ईश्वर एक है” का सिद्धांत दिया और समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव, जातिवाद, और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। वे समानता, धार्मिक सहिष्णुता, और आध्यात्मिक जागृति के लिए कटिबद्ध थे। उनके विचारों ने न केवल सिख धर्म की नींव रखी बल्कि भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार की दिशा भी प्रदान की।
इतिहासकार का कथन:
वर्ड (W. H. McLeod), जो गुरु नानक और सिख धर्म पर विशेषज्ञ थे, उन्होंने गुरु नानक के बारे में कहा था:
“गुरु नानक एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने धार्मिक एकता, सामाजिक समानता और आत्मिक जागरण के महत्व को समझाया। उन्होंने एक नए विचारधारा का प्रसार किया जिसमें सभी मानवों के लिए समानता और प्यार का संदेश था। उनका जीवन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कार्य किया।”
Q.10. सूफी सन्त के प्रमुख सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। इनका जन-जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ?
उत्तर –
सूफी संतों के प्रमुख सिद्धान्त:
सूफी संतों का धर्म और दर्शन मुख्यतः ईश्वर के साथ एकत्व, भक्ति, और प्रेम पर आधारित था। उनके सिद्धान्तों में आत्मज्ञान, साधना, और सच्चे प्रेम का महत्व था। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म में आंतरिक शुद्धता और आत्मा के ईश्वर से मिलन की दिशा पर बल दिया। उनके प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार थे:
ईश्वर के साथ एकता (तवहीद): सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर एक है और उसका स्वरूप निराकार है। वे इस बात में विश्वास करते थे कि मानवता का लक्ष्य ईश्वर के साथ एकात्मता प्राप्त करना है। यह सिद्धान्त तवहीद के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है।
प्रेम और भक्ति: सूफी संतों ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण साधना माना। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम ही आत्मा को शुद्ध और परमात्मा से जोड़ सकता है। इस सिद्धान्त में अल्लाह या ईश्वर से प्रेम की भावनाएँ प्रकट होती हैं।
ध्यान और साधना: सूफी संतों ने आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के संपर्क के लिए ध्यान और साधना को प्रमुख माना। उनका ध्यान विभिन्न तरीकों से किया जाता था, जैसे वज़ीफे, ध्यान-समाधि, और संगीत-भक्ति (काव्वाली), जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और परमात्मा के नजदीक पहुंचाने में मदद करते थे।
विवेकपूर्ण जीवन और साधना: सूफी संतों का मानना था कि एक व्यक्ति को अपने जीवन को शुद्ध और साधारण रखना चाहिए। उन्होंने सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मिक संतुलन और आत्मा के शुद्धिकरण के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।
विनम्रता और सहिष्णुता: सूफी संतों ने जातिवाद, धर्म, और पंथ के भेद को नकारा और यह शिक्षा दी कि सभी मानव जातियाँ समान हैं। वे धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे और उन्होंने सभी धर्मों में समानता और सहिष्णुता का प्रचार किया।
जन-जीवन पर प्रभाव:
सूफी संतों के सिद्धान्तों का जन-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सूफी विचारधारा ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता, और मानवता का आदर्श स्थापित किया। उनके योगदान का असर न केवल मुस्लिम समाज पर पड़ा, बल्कि उनके संदेशों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद और एकता को भी बढ़ावा दिया। सूफी संतों के सिद्धान्तों का भारतीय समाज में निम्नलिखित प्रभाव पड़ा:
धार्मिक सहिष्णुता: सूफी संतों ने हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच सामूहिक विश्वास और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा स्थापित कुल शरीफ जैसे स्थलों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक साथ आते थे और वहाँ की पूजा विधियों को साझा करते थे।
सामाजिक समानता: सूफी संतों ने समाज में व्याप्त जातिवाद, वर्गभेद और भेदभाव को नकारा। उनका संदेश था कि सभी मानव एक जैसे हैं और ईश्वर के दरबार में सब बराबर हैं। इसने समाज में एकता और समानता को बढ़ावा दिया।
भक्ति और प्रेम: सूफी संतों ने व्यक्ति को ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध और प्रेम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इसने लोगों को आत्मिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर किया।
काव्य और संगीत का प्रसार: सूफी संतों का संगीत, खासकर काव्वाली, भारतीय संगीत पर एक गहरी छाप छोड़ गया। यह संगीत न केवल भक्ति का एक रूप था, बल्कि यह समाज में प्रेम, सौहार्द्र और शांति के प्रचार का एक प्रभावी माध्यम बन गया।
आध्यात्मिक जागृति: सूफी संतों ने व्यक्तिगत आत्मा के शुद्धिकरण और आत्मज्ञान पर बल दिया। उनके सिद्धान्तों ने लोगों को आत्मनिरीक्षण, आत्मसाक्षात्कार और मानसिक शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
सूफी संतों के सिद्धान्तों और उनके जीवन के आदर्शों ने भारतीय समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखा, जिसमें धार्मिक आस्थाओं के पार जश्न, प्रेम, और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी गई।
Q.11. सूफीवाद से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर – सूफीवाद उन्नीसवीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका अरबी शब्द ‘तसत्वुफ’ से संबंधित है। सूफीवाद इस्लामिक धर्म में एक आध्यात्मिक पंथ या परंपरा है, जिसका उद्देश्य ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति और आत्म-ज्ञान है। इस शब्द का उपयोग इस्लामी ग्रंथों में किया जाता है, और इसके बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार, ‘सूफी’ शब्द ‘सूफ’ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी संत पहनते थे, जो एक साधारण और तपस्वी जीवन की ओर संकेत करता है। यह इस बात को दर्शाता है कि सूफी अपनी साधना के दौरान भौतिक सुखों से दूर रहते हुए केवल आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं, अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति ‘सफा’ से मानते हैं, जिसका अर्थ है ‘साफ’ या ‘शुद्ध’। इसका मतलब यह हो सकता है कि सूफीवाद शुद्धता, आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की राह पर चलने के दर्शन को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि ‘सूफी’ शब्द ‘सफा’ से उत्पन्न हुआ है, जो पैगम्बर मुहम्मद की मस्जिद के बाहर एक चबूतरे का नाम था। यहाँ पर पैगम्बर के निकटतम अनुयायी इकट्ठा होकर धर्म के विषय में चर्चा करते थे और गहरी धार्मिक शिक्षाएँ प्राप्त करते थे। इस प्रकार, सूफीवाद का महत्व इस्लाम में आंतरिक शुद्धता, प्रेम, और ईश्वर से एकात्मता की प्राप्ति पर आधारित है, और यह जीवन को भौतिक सुखों से परे आत्मिक समृद्धि की ओर अग्रसर करने का एक मार्ग है।
Q.12. ‘भुक्ति’ शब्द का क्या आशय है ?
उत्तर – ‘भुक्ति’ शब्द संस्कृत के ‘भुक्ति’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है ‘भोग’ या ‘आनंद का अनुभव करना’। यह विशेष रूप से धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है और यह संसारिक सुखों, भौतिक आनंद और सम्पत्ति के भोग को दर्शाता है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में ‘भुक्ति’ का उपयोग किसी व्यक्ति के सांसारिक सुखों या भौतिक समृद्धि के अनुभव के लिए किया जाता है। भुक्ति शब्द का उल्लेख विशेष रूप से उन सिद्धांतिक पंथों में किया जाता है जहाँ व्यक्ति सांसारिक सुखों और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म और साधनाओं में संलग्न होता है। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष धार्मिक विचारधाराओं में ‘भुक्ति’ का अर्थ ईश्वर से प्राप्त सांसारिक आशीर्वाद और समृद्धि के रूप में लिया जाता है, जो जीवन के उद्देश्य के रूप में देखा जाता है। इस शब्द को ‘मोक्ष’ (मुक्ति) के विपरीत प्रयोग में लाया जाता है, जहां ‘मोक्ष’ आत्मा की मुक्ति और ईश्वर से एकात्मता का प्रतीक है। ‘भुक्ति’ का अर्थ संसारिक सुखों के भोग के संदर्भ में अधिक होता है, जबकि ‘मोक्ष’ आत्मिक मुक्ति का लक्ष्य होता है।
Q.13. फतेहपुर सीकरी के विषय में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर – 1556 ई. में जब अकबर बादशाह बना, उस समय मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। 1570 ई. में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि अकबर को अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर विशेष आस्था थी, और फतेहपुर सीकरी अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, इसलिए उसने इस स्थान को अपनी नई राजधानी के रूप में चुना। यहाँ अकबर ने सुंदर महल बनवाए और गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इसके अलावा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहाँ बनवाया गया, जो आज भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हालाँकि, फतेहपुर सीकरी मुग़ल साम्राज्य की राजधानी के रूप में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अकबर ने 1585 में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। इसके बावजूद, फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बना हुआ है। यह शहर मुग़ल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
Q.14. खान-ए-खाना के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर – खान-ए-खाना (Khan-a-khana) – “खान-ए-खाना” का शाब्दिक अर्थ है “खानों में सबसे महान”। यह एक उपाधि थी जो अकबर ने अपने संरक्षक और गुरु बैरम खाँ को दी थी। बैरम खाँ अकबर के राजवंश के प्रारंभिक वर्षों में एक प्रमुख व्यक्ति थे और अकबर की आंतरिक तथा बाहरी राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बैरम खाँ अकबर के सिंहासनारोहण के समय उनके संरक्षक थे, क्योंकि उस समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष और 4 महीने थी। बैरम खाँ ने 1556 से 1560 ई. तक अकबर को अपने दिशा-निर्देशों और मार्गदर्शन से राजकार्य चलवाया। उनके मार्गदर्शन में ही अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को स्थिर किया और उसे एक मजबूत नींव दी। बैरम खाँ की सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता के कारण ही अकबर का साम्राज्य पहले की तुलना में मजबूत और समृद्ध हुआ। “खान-ए-खाना” की उपाधि बैरम खाँ को उनकी वीरता, निष्ठा और अकबर के प्रति उनके योगदान के सम्मानस्वरूप दी गई थी। इस उपाधि के द्वारा बैरम खाँ को मुग़ल साम्राज्य में एक प्रमुख और सम्मानित स्थान मिला।
Q.15. अबुल फजल कौन था ? उस पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर – अबुल फजल – अबुल फजल अकबरकालीन महान कवि, निबंधकार, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, सेनापति और आलोचक थे। उनका जन्म 1557 ई. में आगरा के प्रसिद्ध सफी शेख मबारक के यहाँ हुआ था। 1574 ई. में उन्होंने अकबर के दरबार में प्रवेश किया और वह शीघ्र ही अकबर के प्रमुख दरबारियों में शामिल हो गए। उन्होंने कोषाध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक के पदों पर कार्य किया और भारतीय इतिहास में एक महान इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अबुल फजल ने दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की रचनाएँ कीं: ‘अकबरनामा’ और ‘आइने अकबरी’। ये दोनों ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए और अकबर कालीन इतिहास जानने के मुख्य स्रोत बने। ‘अकबरनामा’ अकबर की जीवनी, उसकी विजयों, शासन व्यवस्था के साथ-साथ तत्कालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करता है। ‘आइने अकबरी’ में अकबर के शासन की प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण है। अबुल फजल ने ‘पंचतंत्र’ का फारसी में अनुवाद किया और उसे ‘अनघरे साहिली’ नाम दिया। अकबर के नौ रत्नों में वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्होंने कई सैनिक अभियानों का नेतृत्व भी किया और अकबर के प्रधानमंत्री तथा परामर्शदाता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक दृष्टिकोण से अबुल फजल बहुत उदार थे। उनके विचार सूफी संतों से मिलते-जुलते थे, और उन्हें अकबर द्वारा शुरू किए गए दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाने की प्रेरणा देने का श्रेय दिया जाता है। वह अकबर के इबादतखाने में सूफी मत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे और अकबर के नौ रत्नों में दीन-ए-इलाही को अपनाने वाला वह पहला व्यक्ति थे। अलंकृत जीवन के बावजूद अबुल फजल की मृत्यु बहुत ही त्रासदीपूर्ण रही। उन्हें सलीम ने वीरसिंह बुंदेला के साथ सांठ-गांठ करके मारा था। कहा जाता है कि अबुल फजल की मृत्यु के शोक में अकबर ने तीन दिनों तक दरबार नहीं खोला था। अकबर ने भावुक होकर यह कहा था, “अगर सलीम राज्य चाहता था तो वह मेरी हत्या करवा देता, लेकिन अबुल फजल को छोड़ देता।” आज भी जब तक भारतीय इतिहास में अकबर का नाम रहेगा, तब तक अबुल फजल को याद किया जाएगा। उनका योगदान न केवल इतिहासकार के रूप में, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष विचारक और राज्य के कुशल प्रशासक के रूप में भी अमूल्य रहेगा।

SANTU KUMAR
I am a passionate Teacher of Class 8th to 12th and cover all the Subjects of JAC and Bihar Board. I love creating content that helps all the Students. Follow me for more insights and knowledge.
Contact me On WhatsApp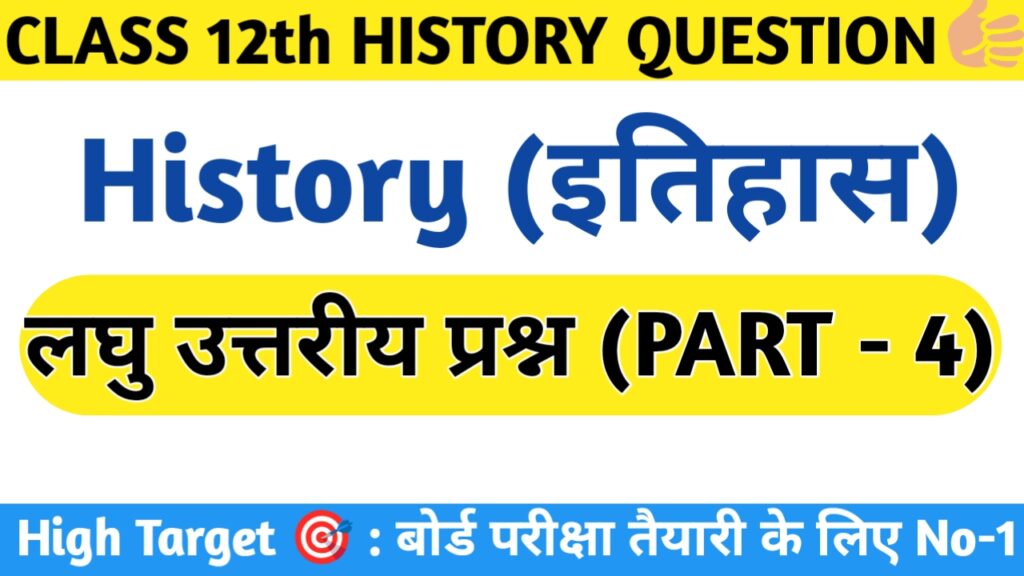
Thanks sir
Thanks for This questions sir, ☺️
Thanks sir 🥰 Please support sir ji , mera v youtube channel h PP Study Point, sab ko bata dijiyega